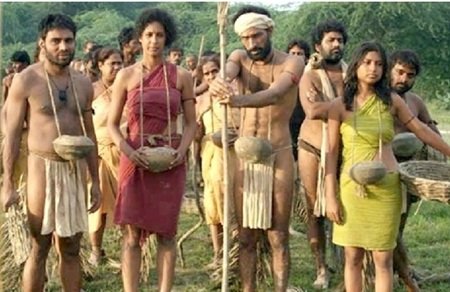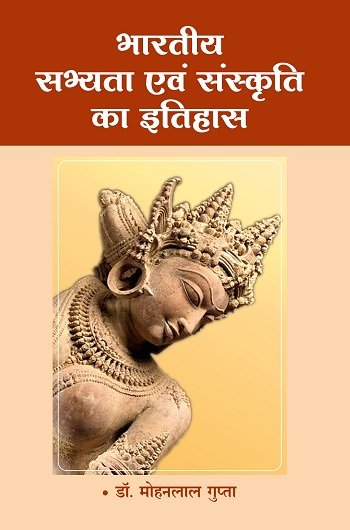चाण्डाल एवं कायस्थ जातियाँ भारतीय जाति प्रथा में तो स्थान रखती हैं किंतु वैदिक आर्य व्यवस्था में इन दोनों जातियों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इससे स्पष्ट है कि ये दोनों जातियाँ वैदिक काल के बाद में अस्तित्व में आईं।
भारतीय इतिहास में चाण्डाल जाति
मनुस्मृति तथा धर्मसूत्रों के अनुसार चाण्डाल जाति की उत्पत्ति शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से हुई थी। महाभारत में इसे नापित पुरुष और ब्राह्मण स्त्री की संतान माना गया है। इसे अत्यधिक हीन तथा महापातकी जाति के अंतर्गत रखा गया है। गौतम के अनुसार ये कुत्ते और कौए की कोटि के थे। आपस्तम्ब की दृष्टि में चाण्डाल को स्पर्श करना, उसे दखेना और उससे बोलना भी पाप था जिसके लिए प्रायश्चित का विधान किया गया था।
छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उसकी स्थिति श्वान और शूकर जैसी थी। माना जाता था कि पूर्वजन्म में असत् कर्म करने के कारण चाण्डाल योनि मिलती थी। बौद्ध काल में भी चाण्डालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। बौद्ध-जातकों से चाण्डालों की हीन एवं दयनीय अवस्था का ज्ञान होता है। मातंग जातक से ज्ञात होता है कि एक चाण्डाल जब नगर में प्रवेश कर रहा था तब एक श्रेष्ठि-दुहिता की दृष्टि उस पर पड़ गई। लड़की ने कहा कि ओह! मैंने तो अशुभ दर्शन कर लिया। इसके बाद अनेक लोगों ने उस चाण्डाल को खूब मारा।
मनु ने लिखा है- ‘चाण्डाल और श्वपच को गांव के बाहर निवास करना चाहिए तथा कुत्ते और गधे उसकी सम्पत्ति होनी चाहिए।’
कफन उसका वस्त्र था। वह फूटे बर्तन में भोजन करता था, उसका अलंकार लोहे का होता था और वह सर्वदा घूमा करता था। उसे रात्रि के समय गांव और नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। वह दिन में राजाज्ञा का विशेष चिह्न धारण करके गांव में घूम सकता था और बान्धव रहित शव को शमशान ले जा सकता था। प्राणदण्ड पाए हुए व्यक्ति का वध करता और उसका वस्त्र, शैया, और आभूषण आदि ग्रहण करता था। पुराणों में भी उसे कुत्ते और पक्षियों की श्रेणी में रखा गया है। श्राद्ध के अन्न पर उसकी दृष्टि पड़ जाने से देवता और पितृगण अपना भाग त्याग देते थे। वह अधम और पातकी था। जो व्यक्ति जानबूझकर चाण्डाल-स्त्री का संग करता था, उसके साथ भोजन करता था या प्रतिग्रह स्वीकार करता था, वह उसी श्रेणी का हो जाता था। चीनी यात्री फाह्यिान (पांचवीं शताब्दी ईस्वी) ने लिखा है कि जब कभी चाण्डाल बाजार में प्रवेश करता था तब वह लकड़ियां बजाता चलता था जिससे लोग लकड़ियों की आवाज सुनकर हट जाएं और उसके स्पर्श से अशुद्ध न हों। वह बहेलिए और मछली मारने का धंधा अपना सकता था। हर्ष के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री ह्वेनत्सांग (सातवीं शताब्दी ईस्वी) ने लिखा है कि वह पशुओं को मारकर उनका मांस बेचता था। बधिक का कार्य करता था, विष्ठा आदि उठाता था और नगर के बाहर रहता था।
उसके घर पर विशेष चिह्न बने होते थे। बाण (सातवीं शताब्दी ईस्वी) ने अपनी पुस्तक कादम्बरी में उसे स्पर्श-वर्जित कहा है। तथा बांस की छड़ी बजाकर अपने आने की सूचना देने वाला निर्दिष्ट किया है। अल्बरूनी (दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी ईस्वी) ने लिखा है कि उसका मुख्य कार्य गांव की सफाई करना था।
अनेक अरब लेखकों ने लिखा है कि वह स्थान-स्थान पर खेल-तमाशे करके जीविकोपार्जन करता था। उसका वर्ग खिलाड़ी और कलावन्त का था। जैन आचार्य हेमचंद्र (बारहवीं शताब्दी ईस्वी) ने लिखा है कि चाण्डाल लकड़ी की आवाज करते हुए चलते थे ताकि उच्च वर्ण के लोग उसे छूने से बच जाएं। कल्हण (बारहवीं शताब्दी ईस्वी) ने भी चाण्डाल की हीन स्थिति का वर्णन किया है।
भारतीय इतिहास में कायस्थ जाति
कायस्थ जाति का उल्लेख भारतीय आर्य वर्ण-व्यवस्था में नहीं मिलता। उनका विकास अलग वर्ग और जाति के रूप में हुआ। प्राचीन भारत में कायस्थों की स्थिति के बारे में अलग-अलग बातें मिलती हैं। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवलक्य ने किया है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कायस्थों को चोर-डाकुओं से अधिक खतरनाक बताया है तथा राजा को आदेश दिया है कि वह कायस्थों से अपनी प्रजा की रक्षा करे।
महर्षि उषनस एवं महर्षि व्यास ने अपनी स्मृतियों में कायस्थों का उल्लेख शूद्र जाति के रूप में उल्लिखित किया है। औशनस स्मृति के अनुसार ‘कायस्थ’ शब्द का निर्माण ‘काल’, ‘यम’ और ‘स्थपति’ के प्रारम्भिक अक्षरों को मिलाकर हुआ है। कायस्थ जाति के सम्बन्ध में गुप्तकालीन अभिलेखीय प्रमाण भी मिलता है। गुप्तकालीन अभिलेख में उन्हें ‘प्रथम कायस्थ’ एवं ‘ज्येष्ठ कायस्थ’ कहा गया है।
सहेत-महेत के गाहड़वाल अभिलेख में कायस्थ शब्द का उल्लेख ‘लेखक’ के रूप में हुआ है जबकि चन्देल, चेदि, चाहमान आदि अभिलेखों में उन्हें कायस्थ जाति एवं कायस्थ वंश कहा है।
अतः अनुमान होता है कि कायस्थ, गुप्त काल तक भारतीय समाज में चारों वर्णों से अलग, एक वर्ग के रूप रह रहे थे और नौवीं शताब्दी आते-आते वे एक जाति में बदल गए। उनका प्रधान कर्म लेखन कार्य करना था। वे लेखाकरण, गणना, आय-व्यय और भूमि-कर के भी अधिकारी होते थे। हरिषेण (दसवीं शताब्दी ईस्वी) ने उनके लिए लेखक एवं कायस्थ दोनों शब्दों का प्रयोग किया है।
श्री हर्ष ने उनकी उत्पत्ति यम के लिपिक चित्रगुप्त से मानी है। ग्वारहवीं सदी के एक अभिलेख में कायस्थ वंश को बहुत पुराना माना गया है तथा उनका उद्भव कुश और उनका पिता काश्यप विवृत है। एक अभिलेख में उनका सम्बन्ध क्षत्रियों से बताया गया है जिसके अनुसार जब परशुराम ने इन निर्भीक क्षत्रियों को समाज से निकाल दिया तब वे ‘कायस्थ’ कहे गए।
कायस्थ अपना उपनाम ‘पंचोली’ भी लिखते हैं जिसका संकेत ‘पांचवे वर्ण’ की ओर प्रतीत होता है। ‘कायस्थ’ और ‘पंचोली’ दोनों ही शब्द इन लोगों के समाज रूपी ‘काया में स्थित होने’ एवं समाज के ‘पांचवे चोले’ में स्थित होने की ओर भी संकेत करते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुस्मृति के रचना काल, छांदोग्य आदि उपनिषदों के रचना काल में फाह्यान आदि चीनी यात्रियों के काल में चाण्डाल एवं कायस्थ जातियों का उल्लेख भारतीय समाज में मिलता है किंतु वैदिक काल में इन जातियों का कोई उल्लेख नहीं हुआ है।
इसका मुख्य कारण यह है कि वैदिक काल में श्रम विभाजन के आधार पर जिस वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था, उस काल में चाण्डाल कर्म तथा कायस्थ जातियों द्वारा किए जाने वाले कर्म की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए वैदिक वर्ण व्यवस्था में चाण्डाल एवं कायस्थ जातियों का उल्लेख नहीं है।
यह भी देखें
चाण्डाल एवं कायस्थ जातियों का जाति प्रथा में स्थान