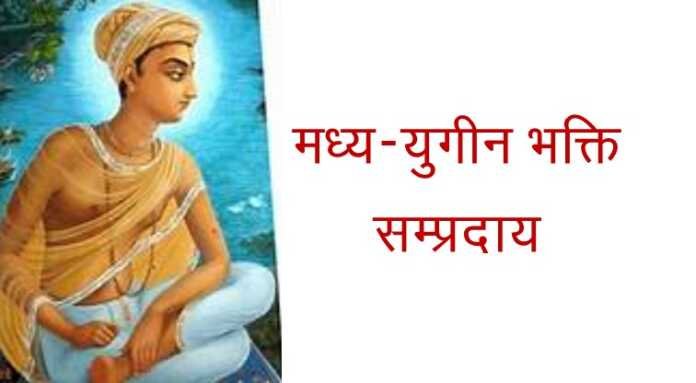मध्य-युगीन भक्ति सम्प्रदाय भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों के प्रति भक्ति भावना रखने के निमित्त स्थापित हुए थे। इन समस्त सम्प्रदायों के मूल दर्शन में भगवान का भक्तवत्सल स्वरूप तथा दुष्ट हंता स्वरूप केन्द्रीय भाव में था, साथ ही भगवान को मोक्ष भक्तों के पापों को दूर करके उन्हें मोक्ष देने वाला भी प्रदर्शित किया गया था।
मध्य-युगीन भक्ति सम्प्रदायों में रामानुजाचार्य का श्री सम्प्रदाय, विष्णु गोस्वामी का रुद्र सम्प्रदाय, निम्बार्काचार्य का निम्बार्क सम्प्रदाय, माधवाचार्य का द्वैतवादी माध्व सम्प्रदाय, रामानंद का विशिष्टाद्वैतवादी रामानन्द सम्प्रदाय, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवादी पुष्टि सम्प्रदाय, चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय सम्प्रदाय अथवा चैतन्य सम्प्रदाय, हितहरिवंश का राधावल्लभी सम्प्रदाय तथा हरिदासी सम्प्रदाय महत्वपूर्ण हैं।
अन्य मध्य-युगीन भक्ति सम्प्रदाय
भक्ति सम्प्रदायों की इस परम्परा में विष्णु गोस्वामी का रुद्र सम्प्रदाय, हितहरिवंश का राधावल्लभी सम्प्रदाय तथा हरिदासी सम्प्रदाय महत्वपूर्ण हैं।
मध्य-युगीन भक्ति सम्प्रदायों की विशेषताएँ
मध्य-युगीन भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तकों ने जिस भक्ति पर जोर दिया, उसका स्वरूप सरल एवं पवित्र था। उसका कोई पुरोहित तथा कर्मकाण्ड नहीं था। भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तकों ने हिन्दू-धर्म के आडम्बरों तथा जटिलताओं को दूर करके उसे सरल तथा स्पष्ट बनाने के प्रयास किए।
इन लोगों ने एकेश्वरवाद एवं अवतारवाद का सहारा लिया तथा ईश्वर की भक्ति विष्णु तथा उनके अवतारों अर्थात् राम एवं कृष्ण के रूप में की गई। हिन्दू-धर्म सुधारकों का विश्वास था कि मोक्ष केवल ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो सकता है। भक्ति-मार्गी सुधारकों ने ‘नाम’ तथा ‘गुरु’ की महत्ता पर बल दिया। उनके उपदेशों में ‘समर्पण’ की प्रधानता है तथा ‘अहंकार’ का अभाव है।
इन सन्तों में से कुछ मूर्तिपूजक थे जबकि कुछ मूर्ति-पूजा को निरर्थक मानते थे परन्तु समस्त संतों ने एक स्वर से जाति-पाँति का विरोध किया तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सुझाया। कुछ संतों ने भक्ति के साथ-साथ प्रपत्ति एवं शरणागति का मार्ग भी सुझाया।
समस्त संतों की मान्यता थी कि ईश्वर किसी स्थान विशेष में नहीं रहकर कण-कण में समाया हुआ है तथा प्रत्येक प्राणी के भीतर निवास करता है। ईश्वर को भक्ति से प्रसन्न एवं अपने वश में किया जा सकता है। प्रायः प्रत्येक संत ने साधक के लिए सच्चे गुरु का होना आवश्यक माना। भक्तिमार्गी सन्तों ने अपने दार्शनिक ग्रंथों की भाषा संस्कृत रखी किंतु उपदेशों एवं भजनों के लिए हिन्दी एवं लोकभाषा को स्वीकार किया।
मुख्य अध्याय – भारत का मध्य-कालीन भक्ति आंदोलन
भक्ति आन्दोलन का पुनरुद्धार एवं उसके कारण
मध्य-युगीन भक्ति सम्प्रदाय