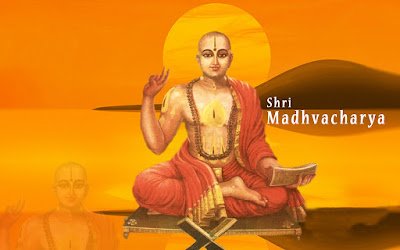दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में माधवाचार्य (ई.1197-1278) वैष्णव परम्परा के बड़े आचार्य हुए। उनका जन्म ई.1197 में कन्नड़ जिले के उडिपी नगर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपनी शारीरिक शक्ति के कारण वे भीम समझे जाते थे। उन्होंने युवावस्था में ही सन्यास ले लिया। वे भी रामानुज की भांति विष्णु के उपासक थे। उन्हें आनंदतीर्थ भी कहा जाता है तथा वायुदेव का अवतार माना जाता है।
माधवाचार्य ने शंकर के अद्वैतवाद का खण्डन करके वैष्णव-भक्ति परम्परा में ‘द्वैतवाद’ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार ब्रह्म, जीव एवं माया तीनों के पृथक् अस्तित्व हैं और तीनों ही अक्षर हैं अर्थात् इनका कभी क्षरण नहीं होता। उन्होंने वेदान्त के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर ‘विष्णु’ की प्रतिष्ठा की।
मध्वाचार्य में वाद-विवाद करने की अद्भुत योग्यता थी। अपने विचारों की पुष्टि के लिए उन्होंने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और अनेक विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। मध्वाचार्य का ‘द्वैतवाद’ का सिद्धान्त रामानुज के ‘विशिष्टाद्वैत’ के सिद्धान्त से काफी मिलता-जुलता है। दोनों ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं और विष्णु को ही ईश्वर मानते हैं।
अन्तर केवल इतना ही है कि रामानुज ने ईश्वर, जगत् और जीव, तीनों को सत्य, नित्य और अनादि माना तथा जीव और जगत् को अनिवार्य रूप से ईश्वर पर आश्रित माना। अर्थात् इनमें विशिष्ट प्रकार का द्वैत है। जबकि मध्वाचार्य जीव और जगत् को ईश्वर से सर्वथा भिन्न मानते हैं। मध्वाचार्य के विचार से अन्य समस्त तत्त्व ईश्वर से भिन्न होते हुए भी उस पर आधारित हैं। केवल ईश्वर की ही अपनी स्वतन्त्र सत्ता है।
मध्वाचार्य का ईश्वर सर्वगुणसम्पन्न है और उसका सम्पूर्ण ज्ञान मानव की शक्ति एवं समझ से परे है। ज्ञान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति सम्भव नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति केवल भक्ति से हो सकती है। इसके लिए निष्काम कर्म, योग्य गुरु का मार्गदर्शन और ईश्वर की उपासना आवश्यक है। उनके विचार में मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य ‘हरि-दर्शन’ प्राप्त करना है। हरि-दर्शन से मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
मुख्य अध्याय – भारत का मध्य-कालीन भक्ति आंदोलन
भक्ति आन्दोलन का पुनरुद्धार एवं उसके कारण
मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत
माधवाचार्य