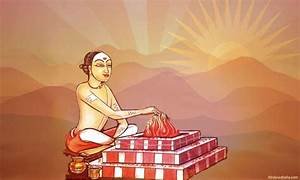पुरुषार्थ-चतुष्टय की अवधारणा मनुष्य के जीवन को संतुलित, सुखी एवं दीर्घ जीवन जीने के लिए है। यह प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्म करते हुए मोक्ष की तरफ ले जाती है। इन्हें पुरुषार्थ भी कहा जाता है।
पुरुषार्थ-चतुष्टय के चार अंग हैं- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से प्रथम पुरषार्थ है- धर्म! धर्म के सम्बन्ध में मनुस्मृति का कथन है- वेद सब धर्मों का मूल है और वेद के जानने वाले लोगों की स्मृति तथा शील भी धर्म के मूल हैं। सत्पुरुषों का सदाचार भी धर्म का मूल है और अन्तरात्मा का संतोष भी धर्म का मूल है।
प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में नाना प्रकार के सुख, सौभाग्य, सफलता एवं समृद्धि प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। इनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ उद्यम करना होता है। मनुष्य के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के सुखों में से कुछ सुख भौतिक हैं, कुछ दैहिक हैं तथा कुछ दैविक अथवा आध्यात्मिक हैं।
संस्कृति के निर्माताओं ने इस बात पर गहनता से विचार किया कि मनुष्य को अपने जीवन में किन सुखों की कामना करनी चाहिए तथा वे कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे ऋषियों ने इस बात पर भी गहन विचार किया कि मनुष्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सुखों में नैतिकता का तत्व किस प्रकार संलग्न रहे। अनीति पूर्वक प्राप्त किए गए सुख, सफलताएं एवं समृद्धि कभी भी किसी भी मनुष्य को अंतिम रूप से सुखी नहीं बना सकते।
ऋषियों ने अनुभव किया कि सांसारिक मोह-माया और भोग-विलास मनुष्य को आकर्षित तो करते हैं किंतु वे मनुष्य को सन्मार्ग की ओर न ले जाकर दुःखों की ओर ले जाते हैं। जबकि मर्यादित आचरण तथा आध्यात्मिक विचार उचित निर्णय लेने में मनुष्य की सहायता करते हैं। भारतीय मनीषियों ने पाया कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्षणिक सुखों की प्राप्ति की बजाए स्थाई सुखों की उपलब्धि होना चाहिए।
मनुष्य की चेष्टाएं विलासपरक न होकर धर्मपरक होनी चाहिए। आध्यात्मिक वृत्तियां मनुष्य को जीवन-दर्शन का वास्तविक अर्थ समझाती हैं जिसमें सांसारिकता के साथ-साथ आध्यात्मिकता, भोग के साथ योग तथा कामना के साथ निवृत्ति का संतुलन रहता है। वस्तुतः मनुष्य को अपने जीवन में दैहिक, दैविक एवं भौतिक, तीनों प्रकार के सुखों की आवश्यकता होती है।
पुरुषार्थ-चतुष्टय
ऋषियों ने इन सुखों को चार प्रकार के ‘पुरुषार्थों’ के रूप में अभिव्यक्त किया। इन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा जाता है। इनमें से ‘काम’ दैहिक सुख है और अर्थ ‘भौतिक सुख’ है, ‘धर्म’ एवं ‘मोक्ष’ दैविक सुख हैं।
इन चार पुरुषार्थों को ‘चतुर्वर्ग’ एवं ‘पुरुषार्थ-चतुष्टय’ भी कहा गया है। पुरुषार्थों से ही मनुष्य बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष करता है। भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के मध्य संतुलन स्थापित करना ही पुरुषार्थ का सही स्वरूप है। ‘धर्म’ के द्वारा मनुष्य नीति, विवेक, न्याय आदि क्रियाओं को समझ सकता है। ‘अर्थ’ मुनष्य की भौतिक समृद्धि का आधार है।
‘काम’ मानव के मन एवं देह को संतुष्टि देता है। इन तीनों के सम्यक् उपभोग से मनुष्य स्वतः ही ‘मोक्ष’ अर्थात् आत्मा की चरम उन्नति प्राप्त कर लेता है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य ‘मोक्ष’ ही है।
चार्वाक दर्शन केवल दो ही पुरुषार्थों- अर्थ और काम को मान्यता देता है। वह धर्म और मोक्ष को नहीं मानता। महर्षि वात्स्यायन भी मनु के पुरुषार्थ-चतुष्टय के समर्थक हैं किन्तु वे मोक्ष तथा परलोक की अपेक्षा धर्म, अर्थ और काम पर आधारित सांसारिक जीवन को सर्वोपरि मानते हैं।
मुख्य अध्याय – पुरुषार्थ-चतुष्टय
पुरुषार्थ-चतुष्टय की अवधारणा