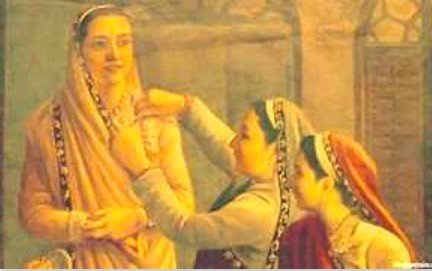मनुष्य जीवन में ‘ काम ‘ को तीसरा पुरुषार्थ माना गया है। इस पुरुषार्थ का भी मनुष्य जीवन में शेष तीनों पुरुषार्थों के समान ही महत्त्व है।
काम के दो स्वरूप हैं- (1.) कामना अर्थात् किसी भी वस्तु अथवा सुख को प्राप्त करने की इच्छा। (2.) यौन-सुख अथवा ऐन्द्रिक-इच्छा। पुरुषार्थ रूपी काम का प्रमुख आशय यौन-इच्छाओं से ही है। यह प्राणी मात्र की सहज प्रवृत्ति है जो उसे प्रकृति से मिली है।
संतान प्राप्ति की इच्छा का कारण भले ही कुछ भी हो किंतु संतान प्राप्ति का माध्यम केवल यौन-इच्छा है। यौन-इच्छा के वशीभूत होकर प्राणी इस संसार चक्र को आगे बढ़ाने में समर्थ हेाता है। यौन-इच्छा के कारण ही मनुष्य पत्नी और सन्तान की कामना करता है। काम-भाव के अंतर्गत यौन-आकर्षण से लेकर स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, अनुराग आदि सम्मिलित होते हैं तथा इस भाव का चरम इन्द्रिय-सुख और यौन-इच्छाओं की तृप्ति है।
‘काम’ मनुष्य जीवन में उत्साह एवं आनंद की सृष्टि करता है तथा उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है किंतु इसका अतिरेक चारित्रिक दुर्बलता एवं महान् दुर्गुण माना जाता है। इसलिए काम का सेवन भी अर्थ की भांति धर्मानुकूल होना चाहिए। सामाजिक मर्यादाओं के बंधन में रहे बिना यौन-इच्छा की पूर्ति, व्यक्ति एवं सम्पूर्ण मानव समाज को हीन अवस्था में पहुँचा सकती है तथा उन्हें पशुवत् बना सकती है। अतः काम पर धर्म के बंधन के साथ-साथ सामाजिक मर्यादाओं का भी अंकुश होना चाहिए।
महाभारत में कहा गया है कि ‘धर्म’ सदा ही ‘अर्थ’ प्राप्ति का कारण है और ‘काम’, ‘अर्थ’ का फल है। कौटिल्य ने काम को अन्तिम श्रेणी में रखा है तथा बिना धर्म और अर्थ को बाधा पहुँचाये इसका पालन करने का निर्देश दिया है। मनु ने ‘काम’ को ‘तमोगुण’ माना है। यौन-इच्छा को मनुष्य का अन्तिम उद्देश्य मानकर, धर्म और अर्थ की प्राप्ति के बाद ही इसकी ओर देखना चाहिए। फिर भी काम को धर्म का सार माना गया है क्योंकि व्यक्ति की समस्त अन्तर्वृतियाँ ‘कामना‘ से संचालित होती हैं।
यौन-इच्छा के तीन मुख्य आधार माने गए है- जैविकीय, सामाजिक और धार्मिक। व्यक्ति अपनी ‘ऐन्द्रिक-इच्छाओं’ अर्थात् वासनाओं की पूर्ति जैविकीय आधार पर करता है। ऐन्द्रिक-इच्छाओं की तृप्ति न होने पर मनुष्य में निराशा, तनाव, आक्रोश और क्रोध उत्पन्न होता है। जबकि इनकी पूर्ति से व्यक्ति के मन में तृप्ति का भाव आता है। उसके मन को पूर्णता प्राप्त होती है एवं उसके अहंकार की भी पूर्ति होती है। ऐसा मनुष्य संयत्, शीलयुक्त एवं मर्यादित आचरण करता है।
इच्छाओं से तृप्त व्यक्ति धर्म का अनुसरण करता है तथा अंत में ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करता है जबकि काम-इच्छाओं की पूर्ति न होने से मनुष्य, ‘कामाग्नि’ में झुलसता रहता है। कामेच्छा पूरी किए बिना उसे दूसरी वस्तुओं की कामना नहीं रह जाती। इसलिए कौटिल्य ने लिखा है- ‘मनुष्य को धर्म, अर्थ और काम का समान भाव से सेवन करना चाहिए।’ इनमें से किसी एक को अपनाने एवं अन्य पुरुषार्थों की उपेक्षा करने से मनुष्य का चिंतन, दृष्टिकोण एवं व्यवहार असंतुलित हो जाते हैं।
अनेक विद्वानों द्वारा ‘काम’ को मात्र ‘यौन-सुख’ मानने की प्रवृत्ति की कटु आलोचना हुई तथा ‘कामना’ को भी ‘काम’ माना गया। यदि ‘काम’ सृष्टि का मूल है तो ‘कामना’ जीवन का आधार है। कामना-रहित जीवन, संभव नहीं है। कामना का मूल मनुष्य के ‘मन’ में ‘कामना‘ से विराजमान है।
इसीलिए काम को ‘मनोज’ अर्थात् ‘मन से जन्म लेने वाला’ कहा गया है। ‘काम’ से ही मन में विविध ‘कामनाएँ’ उत्पन्न होती हैं। किसी कामना के उदय होने पर ही हम किसी कार्य को करने के लिए उद्यत होते हैं और उस ‘उद्यम’ का फल कामनाओं की पूर्ति के रूप में प्राप्त होता है।
प्राचीन ऋषिगण किसी न किसी कामना से संयुक्त होकर तपस्या करते थे। कामना के वशीभूत होकर ही ब्राह्मण वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन करते थे। कामना से ही मनुष्य श्राद्धकर्म, यज्ञकर्म, दान और प्रतिग्रह में प्रवृत्त होता है। व्यापारी, कृषक, शिल्पी तथा कर्मकार भी किसी न किसी कामना से ही अपने-अपने कर्मों में प्रवृत होते हैं।
बिना कामना के ब्राह्मण भी अच्छे अन्न का भोजन नहीं करते और न ही कोई बिना कामना के ब्राह्मणों को दान देता। मनु ने न तो कामुकता को प्रशंसनीय माना है और न ही काम-विहीन अवस्था को। यदि केवल ‘कामना-विहीनता’ को स्वीकार किया जाए तो सत् कार्यों के मूल में निहित काम का भी परित्याग करना पड़ता है।
मुख्य अध्याय – पुरुषार्थ चतुष्टय
काम – पुरुषार्थ-चतुष्टय (3)