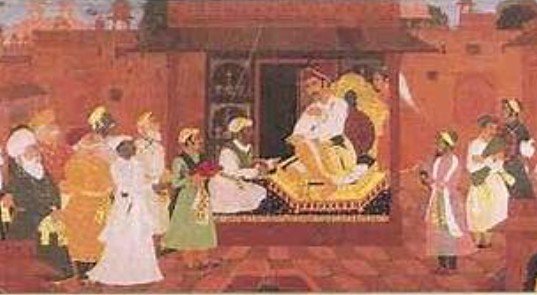दीन-ए-इलाही का शाब्दिक अर्थ, ‘ईश्वर का धर्म’ होता है परन्तु वास्तव में दीन-ए-इलाही कोई धर्म नहीं था। यह ऐसे लोगों की एक गोष्ठी थी जो अकबर के विचारों तथा विश्वासों से सहमत थे और जो उसे अपना पीर या गुरु मानने को तैयार थे।
अकबर जानता था कि न तो समस्त धर्मों को जोड़कर एक किया जा सकता है और न नया धर्म चलाया जा सकता है परन्तु वह अपने विचारों तथा विश्वासों को उन लोगों में प्रचलित करना चाहता था जो उनका स्वांग करना चाहते थे। फलतः अकबर ने उन लोगों की एक गोष्ठी बनाने का निश्चय कर लिया जो उसके धार्मिक विचारों तथा आध्यात्मिक सिद्धान्तों से प्रभावित थे और उसे पीर या गुरु मानकर उसके पद चिह्नों पर चलने के लिए को तैयार थे। इसी गोष्ठी का नाम दीन-ए-इलाही पड़ गया। इसे दीन-इलाही भी कहा जाता था।
दीन-ए-इलाही की स्थापना
दीन-इलाही के सदस्य
दीन-इलाही की सदस्यता अत्यन्त सीमित थी। अकबर जानता था कि उसे प्रसन्न करने अथवा अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये बहुत बड़ी संख्या में लोग इसका सदस्य बनने के लिए उद्यत हो सकते थे। अकबर नहीं चाहता था कि लोग भय अथवा प्रलोभन वश इसके सदस्य बनें।
बदायूनी भी इस बात को स्वीकार करता है कि दीन-ए-इलाही का सदस्य बनाने के लिए धन अथवा शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। एक भी ऐसा उदाहरण उपलब्ध नहीं है कि दीन-इलाही का सदस्य बनने से किसी के पद में वृद्धि हुई हो अथवा इसका सदस्य बनने से मना कर देने पर किसी प्रकार की क्षति पहुँची हो अथवा दण्ड मिला हो।
इसमें केवल वही लोग सम्मिलित हो सकते थे जो स्वेच्छा से इसका सदस्य बनना चाहते थे और जिन्हें अकबर इसका सदस्य बनने योग्य समझता था। बिना अकबर की स्वीकृति के कोई इसका सदस्य नहीं बन सकता था। इतने सारे प्रतिबन्धों के होते हुए भी कई हजार लोग इसके सदस्य बन गये।
अब लगभग बीस सदस्यों के नाम उपलब्ध हैं। बीरबल के अतिरिक्त शेष समस्त सदस्य मुसलमान थे। इनमें से कुछ बड़े ही योग्य, चरित्रवान् तथा स्वतन्त्र विचार के व्यक्ति थे। राज्य के बड़े-बड़े हिन्दू मंत्रियों में से, जो अकबर के बड़े विश्वासपात्र थे, यथा भगवानदास, मानसिंह, टोडरमल आदि कोई भी दीन-ए-इलाही का सदस्य नहीं बना।
सदस्य बनने की प्रक्रिया
दीन-इलाही का सदस्य बनने के लिए अकबर ने रविवार को दीक्षा देने का दिन निर्धारित किया। उसी दिन लोग इसके सदस्य बन सकते थे। जो व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता था वह अपने हाथों में एक पगड़ी लेकर अपने सिर को अकबर के चरणों पर रख देता था। अकबर उसे उठाकर उसकी पगड़ी उसके सिर पर रख देता था।
तब अकबर शिस्त शब्द का उच्चारण करता था। शिष्य भी इस शब्द को दोहराता था। शिस्त शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है- कटिया, जिससे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं या कटिया लगाना परन्तु यहाँ पर इसका अर्थ है शिष्यता ग्रहण करना। एक पत्र पर शिस्त शब्द अंकित रहता था जिस पर ‘अल्ला-हो-अकबर’ अर्थात् ईश्वर महान् है भी लिखा रहता था। नये शिष्य को अकबर का एक लघु चित्र भी मिलता था जिसे वह प्रायः अपनी पगड़ी में रखता था।
सिद्धांत
दीन-इलाही के सदस्यों को निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना होता था-
(1.) दीन-इलाही के सदस्य आपस में मिलने पर अल्ला-हो-अकबर अर्थात् ‘ईश्वर महान् है’ कहकर प्रणाम करते थे और जल्ला-जलाल-हू अर्थात् ‘महान् है उसका ऐश्वर्य’ कहकर प्रणाम का उत्तर देते थे।
(2.) दीन-इलाही के सदस्यों को मांस-भक्षण से बचने का यथा-सम्भव प्रयत्न करना चाहिये था और अपने जन्म के महीने में तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिये था।
(3.) वन्ध्या, गर्भवती स्त्रियों तथा रजस्वला होने के पूर्व कन्याओं के साथ मैथुन करने का निषेध था।
(4.) दीन-इलाही का न कोई धर्मग्रन्थ था, न कोई आचार्य थे, न कोई देवालय या पूजागृह था और दीक्षा के अतिरिक्त न कोई त्यौहार या अनुष्ठान था।
(5.) बदायूनी ने लिखा है कि दीन-ए-इलाही के अनुयायियों को लिखित वचन देना पड़ता था कि वे इस्लाम को त्याग देंगे।
(6.) त्याग की चार कोटियाँ थीं- सम्पत्ति का त्याग, जीवन का त्याग, सम्मान का त्याग तथा धर्म का त्याग।
दीन-इलाही के उद्देश्य
अकबर द्वारा दीन-ए-इलाही को आरम्भ करने के निम्नलिखित उद्देश्य थे-
(1.) अकबर किसी नये धर्म का प्रचार नहीं करना चाहता था और न किसी धर्म को नष्ट करना चाहता था। वह घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, कलह तथा पारस्परिक संघर्ष के जगत् में प्रेम, सहयोग तथा सद्भावना का राज्य स्थापित करना चाहता था।
(2.) अकबर अपने राज्य से वैचारिक संकीर्णता तथा धार्मिक असहिष्णुता को दूर करके सब लोगों में सुलह, शान्ति तथा सद्भावना स्थापित करना चाहता था।
(3.) अकबर की धारणा थी कि लोग अपने-अपने धर्म का पालन करते हुए भी कुछ समान आदर्शों तथा सिद्धान्तों के सूत्र में बंधकर भ्रातृत्व का संचार कर सकते थे।
(4.) अकबर अपने चिंतन तथा सत्संग से कुछ महान् आदर्शों का सृजन कर सका था, उन्हें वह अपने व्यावहारिक जीवन में चरितार्थ करके दिखाना चाहता था।
(5.) अकबर प्रजा की राजभक्ति को सुदृढ़ बनाना चाहता था।
दीन-इलाही का महत्व
(1.) अकबर की मृत्यु के साथ ही दीन-ए-इलाही समाप्त हो गया परन्तु अकबर ने जिन आदर्शों तथा सिद्धान्तों को स्थापित किया, उसके वंशज दो पीढ़ियों तक उनका पालन करते रहे।
(2.) शहजादा खुसरो तथा शहजादा दारा अकबर की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते रहे। यदि राज-सत्ता उनके हाथों में चली गई होती तो अकबर की विचारधारा आगे भी जीवित रहती।
(3.) राजनीतिक दृष्टि से दीन-इलाही को विशेष महत्त्व नहीं है क्योंकि बहुत थोड़े से लोग ही इसके सदस्य बने परन्तु इसने एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जिसका ईश्वर तथा अकबर में ध्रुव विश्वास था और जो अकबर के लिये अपना सर्वस्व निछावर करने के लिये उद्यत था।
(4.) दीन-ए-इलाही ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक मतभेद होते हुए भी लोगों के लिये यह सम्भव था कि वे ईश्वर तथा बादशाह की सेवा एक सूत्र में बँध कर करें।
(5.) यदिदीन-ए-इलाही सफल हुआ होता तो यह जन सामान्य में अकबर के प्रति अटल विश्वास उत्पन्न कर देता।
(6.) औरंगजेब के बादशाह बनते ही मुगल शासकों में उदारता का विलोपन हो गया तथा राज्य से दीन-ए-इलाही का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया।
दीन-ए-इलाही की आलोचना
(1.) मुस्लिम तथा ईसाई इतिहासकारों ने दीन-इलाही की तीव्र आलोचना की है। बदायूनी के अनुसार दीन-ए-इलाही का प्रचार इस्लाम को नष्ट करने के लिये किया गया था।
(2.) विन्सेन्ट स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता का द्योतक बताया है। स्मिथ के अनुसार दीन-ए-इलाही, अकबर के हास्यास्पद दम्भ तथा अनियन्त्रित अधिनायकतन्त्र के दानवीय विकास का फल था।
(3.) हेग ने लिखा है- दीन-ए-इलाही वास्तव में लज्जाजनक असफलता रही। वह हिन्दू, मुसलमान तथा ईसाई किसी को भी अच्छा नहीं लगा।
दीन-इलाही की प्रशंसा
अधिकांश हिन्दू इतिहासकारों ने दीन-ए-इलाही की प्रशंसा की है। डॉ. ईश्वरी प्रसाद ने दीन-इलाही की प्रशंसा करते हुए लिखा है- ‘यह एक ऐसा धर्म था जिसमें समस्त धर्मों के गुण विद्यमान थे। इसमें रहस्यवाद, दर्शन तथा प्रकृति पूजा के तत्त्व संयुक्त थे। यह तर्क पर आधारित था। इसने किसी अन्ध-विश्वास को नहीं अपनाया, किसी ईश्वर या पैगम्बर को स्वीकार नहीं किया। अकबर ही इसका मुख्य प्रवर्तक था।’
प्रो. श्रीराम शर्मा ने लिखा है- ‘दीन-इलाही अकबर की राष्ट्रीय आदर्श की उच्च-कोटि की अभिव्यंजना थी।’
एक अन्य इतिहासकार ने लिखा है- ‘जो लोग अकबर की धार्मिक खोज में यह देखते हैं कि उसने राजनीतिक ध्येय से एक ऐसे धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया जिसमें उसकी प्रजा एकता के सूत्र में बँध जाती, वे सत्य के केवल धरातल को ही देख सके हैं और वे भी बिनयॉन की भाँति उस व्यक्ति के अन्तःस्थल तक नहीं पहुँच सके हैं।’
मूल आलेख – मुगल सल्तनत की पुनर्स्थापना – जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर
अकबर के शासन सम्बन्धी उद्देश्य
दीन-ए-इलाही