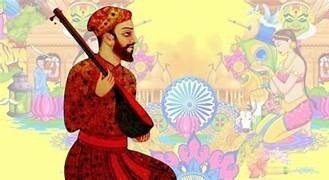भारत का मध्यकालीन साहित्य दो धाराओं में बंटा हुआ है। पहली धारा विदेशी आक्रांताओं की संस्कृति से अनुप्राणित है तथा दूसरी धारा विदेशी आक्रांताओं के संत्रास से से ग्रस्त हिन्दू प्रजा के मनोबल को ऊंचा उठाने उद्देश्य से लिखे गए साहित्य की है।
फारसी साहित्य
अधिकांश तुर्क शासक साहित्य प्रेमी थे और विद्वानों तथा कवियों के आश्रयदाता थे। अतः मध्ययुगीन भारत में महत्त्वपूर्ण साहित्यिक उन्नति हुई किन्तु अधिकतर साहित्य अरबी और फारसी भाषाओं में लिखा गया। इस काल का अधिकांश साहित्य इस्लामिक एवं विभिन्न सूफी मतों से सम्बन्धित है।
अलबरूनी
महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों के समय उसके साथ कई कवि और लेखक भारत आए। अलबरूनी भी उन्हीं में से एक था। उसने संस्कृत भाषा एवं साहित्य का ज्ञान भी प्राप्त किया। उसने अपनी पुस्तक ‘तहकीकाते हिन्द’ में भारत की तात्कालिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। भारत विषयक ज्ञान की गहराई और विस्तार में कोई भी अन्य मुसलमान लेखक अलबरूनी की बराबरी नहीं करता।
मिनहाज-उस-सिराज
इतिहासकार मिनहाज-उस-सिराज इल्तुतमिश के काल में शाही सेवा में था। उसने ‘तबकात-ए-नासिरी’ लिखी जिसमें प्रारम्भिक काल से लेकर 1260 ई. तक का इतिहास है। यद्यपि उसकी गद्य शैली प्रभावपूर्ण नहीं है तथापि घटनाओं की स्पष्टता के कारण ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।
बलबन कालीन साहित्यकार
जब मंगोलों ने मध्य एशियन देशों को विध्वस्त कर डाला, तब इन देशों के मुस्लिम विद्वान् और कवियों ने भागकर दिल्ली में बलबन के दरबार में आश्रय लिया। इस प्रकार दिल्ली में फारसी साहित्य के इतिहास के एक नये युग का सूत्रपात हुआ। बलबन का ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद अच्छे कवियों का बड़ा आदर करता था। फारसी के दो महान् कवियों- अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी ने उसी के आश्रय में काव्य-सृजन आरम्भ किया था।
अमीर खुसरो
अमीर खुसरो फारसी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि था। उसका जन्म 1253 ई. में उत्तर प्रदेश के वर्तमान इटावा जिले के पटियाली गाँव में हुआ था। उसका पिता सैफुद्दीन महमूद एक तुर्क था जो नासिरूद्दीन मुहम्मद के काल में भारत में आकर बस गया था और बाद में इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल में उच्च प्रशासनिक पदों पर रहा।
अमीर खुसरो की माँ बलबन के एक अमीर इमादउलमुल्क की पुत्री थी। खुसरो में काव्य प्रतिभा बचपन से ही थी। उसने आठ वर्ष की आयु में कविता लिखना आरम्भ किया और 12 वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते परिपक्व कवि बन गया। उसने फारसी काव्य से प्रेरणा प्राप्त की। धीरे-धीरे उसने स्वयं अपनी शैली का विकास कर लिया।
वह समस्त प्रकार की काव्य-रचना बड़ी सुगमता से कर लेता था। गीत लिखने में उसे विशेष दक्षता प्राप्त थी। तुर्की, फारसी और हिन्दी भाषाओं पर उसका पूर्ण अधिकार था। खुसरो ने कविता, कहानी, मनसवी और इतिहास के अनेक ग्रन्थ लिखे। उसके कुछ महत्त्वूपर्ण ग्रन्थ हैं- शीरी एवं फरहाद, लैला एवं मजनूं, आइने सिकन्दरी, हश्त-विहिश्त, देवलरानी एवं खिज्रखाँ, तुगलकनामा, तारीखे दिल्ली आदि।
अमीर खुसरो, बलबन से लेकर गियासुद्दीन तुगलक के समय तक कई सुल्तानों के दरबार में रहा। वह सूफी सन्त निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। वह प्रथम भारतीय मुसलमान लेखक था जिसने हिन्दी शब्द और मुहावरों का प्रयोग किया और भारतीय विषयों पर लिखा।
वह उच्चकोटि का कवि, कहानीकार और इतिहासकार होने के साथ-साथ संगीतकार भी था। उसने अपनी कविताओं, पहेलियों और गजलों में हिन्दी और फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया। सूफी होने के कारण उसका दृष्टिकोण उदार था। उसने भारतीय विषयों पर भी लिखा।
अपनी प्रसिद्ध मसनवी ‘नूह सिफ’ (नौ आकाश) में उसने भारतीय जलवायु, पशु, पक्षी, धार्मिक विश्वासों और जन-भाषा का उल्लेख किया। मिनहाज-उस-सिराज की तरह उसने भी भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की। वह भारतीय भूमि की ऊर्वरता, समशीतोष्ण जलवायु और मोरों की प्रशंसा करता है।
कहीं-कहीं तो वह भारत को विश्व के अन्य देशों से श्रेष्ठ ठहराता है। खुसरो भारतीय संगीत का बड़ा प्रेमी था। उसका कहना था कि भारतीय संगीत में विशेष आकर्षण है। माना जाता है कि अमीर खुसरो ने भारतीय वीणा और ईरानी तम्बूरे को मिलाकर सितार का आविष्कार किया।
मीर हसन देहलवी
सुप्रसिद्ध भारतीय मुसलमान कवि मीर हसन देहलवी, अमीर खुसरो का समकालीन और उसका मित्र था। वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवियों में से था तथा अपनी गजलों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। गजलों के कारण वह हिन्दुस्तानी सादी कहलता था। मीर हसन भी निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था।
उसने औलिया के वार्तालापों को अपने फवायद-उल-फौद नामक ग्रन्थ में उल्लेखित किया है। यह ग्रन्थ सूफी दर्शन का अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी उसकी काव्य प्रतिभा से बड़ा प्रभावित हुआ था। उसकी मृत्यु, अमीर खुसरो की मृत्यु के दो वर्ष बाद 1327 ई. में हुई थी।
तुगलक कालीन साहित्यकार
तुगलक शासकों के काल में कई महत्वर्पूण ग्रंथ रचे गये जिनसे उस काल के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उनमें से कुछ इतिहासकारों का परिचय इस प्रकार से है-
जियाउद्दीन बरनी
मुस्लिम इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी मुहम्मद-बिन-तुगलक के दरबार में 17 वर्ष तक रहा। उसने अपने ग्रन्थ का नाम अपने अन्तिम आश्रयदाता फीरोजशाह तुगलक के नाम पर ‘तारीख-ए-फीरोजशाही‘ रखा। इस ग्रन्थ में सुन्दर भाषा का प्रयोग हुआ है।
यद्यपि वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था किन्तु अपने अनुदार दृष्टिकोण के कारण उसने उदार सुल्तानों की बड़ी निन्दा की है। अपने विरोधियों की चालों के कारण फीरोज तुगलक के काल में वह राज्याश्रय से वंचित हो गया। इस कारण उसने अपने अन्तिम वर्ष बड़ी निर्धनता में काटेे।
बदरूद्दीन मुहम्मद
मुहम्मद-बिन-तुगलक के दरबार में एक अन्य विद्वान चय (ताशकन्द) निवासी बदरूद्दीन मुहम्मद भी था। उसके दो ग्रन्थ- ‘दीवान‘ और ‘शाहनामा‘ प्रसिद्ध हैं।
इसामी
इसामी इस युग का प्रसिद्ध विद्वान था उसने ‘फुतूह-उल-फसलातीन’ नामक पद्यबद्ध ग्रन्थ लिखा जिसमें गजनवियों के काल से लेकर 1350 ई. तक के भारत के मुसलमान शासकों का इतिहास है।
फीरोज तुगलक
सुल्तान फीरोज तुगलक स्वयं भी इतिहास लेखन से प्रेम करता था। उसने ‘फतूहात-ए-फीरोजशाही’ नामक ग्रन्थ लिखा जिसमें उसने अपने राज्यकाल का विवरण दिया है।
शम्ससिराज अफीफ
फीरोज तुगलक के समय में शम्ससिराज अफीफ ने ‘तारीखे फीरोजशाही’ नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखा।
मुहम्मद बिहामदखानी
तुगलक शासकों के अन्तिम काल में मुहम्मद बिहामदखानी ने ‘तारीखे मुहम्मदी’ लिखी।
शाइया-बिन-अहमद
शाइया-बिन-अहमद ने तुगलक शासकों के अन्तिम काल में ‘तारीखे मुबारकशाही’ लिखी।
सैयद और लोदी काल के साहित्यकार
सैयद और लोदी काल में भी फारसी साहित्य की प्रगति हुई। इस काल में रफीउद्दीन शीराजी, शेख अब्दुल्ला तुलावनी, शेख जमालुद्दीन के नाम उल्लेखनीय हैं। चौदहवीं सदी के अन्तिम चतुर्थांश में औषधि-शास्त्र, ज्योतिष, संगीत आदि के कुछ उपयोगी संस्कृत ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद किया गया।
फारसी विद्वानों ने मुख्य रूप से साहित्य, इतिहास और धर्म पर ग्रन्थ लिखे थे। इस काल में ऐतिहासिक ग्रन्थ अधिक लिखे गये, जिनमें इतिहासकारों ने अपने आश्रयदाता के शासन की घटनाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया। फिर भी इन ग्रन्थों से सल्तनकालीन इतिहास की अच्छी सामग्री प्राप्त हो जाती है।
प्रांतीय शासकों के समय के साहित्यकार
तुगलक वंश के पतन के बाद भारत में जो प्रान्तीय राज्य स्थापित हुए उनमें भी मध्यकालीन साहित्य विशेषकर फारसी साहित्य की अच्छी प्रगति हुई। दक्षिण के बहमनी वंश के शासकों में से कई स्वयं अच्छे विद्वान थे। सुल्तान ताजुद्दीन फीरोजशाह ज्योतिष का विद्वान् था। उसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई।
गुजरात के महमूद बेगड़ा के शासन काल में फजालुल्लाह जैनुल ओबिदीन ने प्रारम्भ से लेकर नौवीं सदी तक का इतिहास लिखा। बीजापुर के महमूद अयाज ने कामशास्त्र पर ग्रन्थ लिखा जिसमें विभिन्न प्रकार की स्त्रियों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है।
संस्कृत साहित्य
दिल्ली के सुल्तानों ने संस्कृत साहित्य को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। राजकीय संरक्षण नहीं मिलने पर भी मध्यकालीन साहित्य में संस्कृत साहित्य की वृद्धि होती रही। इस युग के अधिकांश संस्कृत ग्रन्थ विजयनगर, वारंगल, गुजरात और राजपूताने के हिन्दू राजाओं के संरक्षण में लिखे गये।
कुछ संस्कृत ग्रन्थों की रचना बंगाल और दक्षिण भारत के भक्ति आन्दोलन के कारण भी हुई। इस काल के ऐतिहासिक काव्य ग्रन्थों में कल्हण कृत ‘राजतंरगिणी‘, न्यायचन्द्र का ‘हम्मीर काव्य’ और सोमचरित गुणी का ‘गुरु गुण रत्नाकर‘ उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं। जयदेवकृत ‘गीत गोविन्द‘ इसी काल की रचना है।
इस काल में संस्कृत नाटक भी बड़ी संख्या में रचे गये। अलबरूनी संस्कृत का ज्ञाता था। उसने संस्कृत के कई ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद करके संस्कृत ग्रंथों के उपयोगी ज्ञान की जानकारी फारसी भाषा के पाठकों तक पहुंचाई।
हिन्दी साहित्य
तुर्की सुल्तानों का हिन्दी भाषा के प्रति कोई लगाव नहीं था किंतु इस काल में मध्यकालीन साहित्य में चले भक्ति आन्दोलन के अनेक सन्तों ने अपने मत का प्रचार करने के लिए हिन्दी भाषा का सहारा लिया। रामानुज और रामानन्द ने भी हिन्दी भाषा में प्रचार किया। राजपूत शासकों की शौर्य गाथाएँ- पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमाण रासो, आल्हा-ऊदल आदि ग्रन्थ हिन्दी भाषा के अन्य रूप डिंगल में लिखे गये।
अमीर खुसरो ने अनेक रचनाओं का हिन्दी भाषा में सृजन किया। खुसरो के समकालीन गोपाल नायक ने हिन्दी की ही एक बोली बृजभाषा में ध्रुपद के गीतों की रचना की। मौलाना दाऊद ने हिन्दी के एक अन्य रूप अवधी में ‘चन्दायन’ की रचना की और कुतबन ने ‘मृगावती’ लिखी। ये दोनों, प्रेम कथाएँ हैं।
उर्दू साहित्य
सल्तनतकाल अथवा उससे थोड़ा पहले मध्य एशियन तुर्कों और हिन्दुओं के सम्पर्क के फलस्वरूप उर्दू भाषा का विकास हुआ। आरम्भ में इसे ‘जबान-ए-हिन्दवी‘ कहा जाता था। बाद में इसे उर्दू कहने लगे। इस भाषा का व्याकरण भारतीय है तथा शब्दावली अरबी एवं फारसी है।
अमीर खुसरो पहला मुसलमान कवि था जिसने इस भाषा को अपनी कविता का माध्यम बनाया। तेरहवीं और चौदहवीं सदी की जनभाषा ‘जबान-ए-हिन्दवी’ ही थी। इसलिए सूफी सन्तों और भक्ति आन्दोलन के कुछ सन्तों ने उर्दू में अपने मत का प्रचार किया। सल्तनतकालीन दिल्ली के सुल्तानों ने उर्दू को प्रश्रय नहीं दिया।
मुगलकाल में भी 18वीं सदी के मध्य तक इसे कोई दरबारी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार तेरहवीं सदी के प्रारंभ से लेकर अठारहवीं सदी के मध्य भाग तक फारसी ही दरबारी भाषा बनी रही।
मुख्य आलेख – मध्यकालीन कला एवं साहित्य
मध्यकालीन साहित्य