दसवीं शताब्दी ईस्वी के अंत में आए मुस्लिम लेखक अलबिरूनी ने मध्यकालीन हिन्दू रीति-रिवाज पर टिप्पणी करते हुए लिखा है- हिन्दू अलग-अलग बैठकर भोजन खाते हैं और उनके भोजन का स्थान गोबर से लिपा चौका होता है। वे उच्छिष्ट का उपयोग नहीं करते हैं और जिन बर्तनों में खाते हैं, यदि वे मिट्टी के होते हैं तो भोजन खाकर बर्तन फैंक देते हैं।
मध्यकालीन हिन्दू रीति-रिवाज प्राचीन काल में विसित हुई सामाजिक संस्थाओं का ही विकसित रूप था। इस काल के जन-जीवन में जाति, कुटुम्ब, विवाह, सोलह संस्कार, दान-पुण्य, हरि-कीर्तन, तीर्थ सेवन आदि परम्पराओं का महत्त्वपूर्ण स्थान था किन्तु इस काल में भारतीय समाज हिन्दू और मुसलमान के रूप में पूरी तरह दो हिस्सों में विभक्त था।
दोनों के सामाजिक नियमों तथा व्यवहार में बहुत अन्तर था। मुसलमानों में बराबरी और भाईचारे का सिद्धान्त था जबकि हिन्दुओं में जाति-प्रथा और छुआछूत के कारण समाज के भीतर भारी विषमता थी। हिन्दुओं एवं मुसलमानों में विवाह से लेकर उत्तराधिकार के नियमों, मृतकों के संस्कार, वेशभूषा, भोजन और स्वागत के ढंग पूरी तरह अलग-अलग थे। दोनों के तीज-त्यौहार एवं पर्व भी अलग-अलग थे।
हिन्दुओं एवं मुसलमानों दोनों में विवाह का निर्णय यद्यपि पारिवारिक होता था किंतु मुसलमानों में उसका आधार जातीय न होकर सामाजिक हैसियत होता था जबकि हिन्दुओं में विवाह का आधार जाति एवं सामाजिक हैसियत दोनों होता था। हिन्दुओं में सहभोज केवल अपनी जाति के लोगों के बीच होता था जबकि मुसलमानों में सहभोज का कोई आधार नहीं था।
हिन्दुओं में विधवा-विवाह अब भी अच्छा नहीं माना जाता था तथा विधवा-विवाह न के बराबर होते थे किंतु मुसलमानों में विधवा-विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं था। हिन्दुओं में विवाह के बाद विच्छेद का कोई तरीका नहीं था किंतु मुसलमानों में पुरुषों द्वारा बड़ी आसानी से तलाक दिया जा सकता था। हिन्दू एक विवाह करते थे किंतु मुसलमान चार विवाह तक कर सकते थे। शहजादे एवं बादशाह कितने भी विवाह कर सकते थे। हिन्दुओं एवं मुसलमानों की संगीत कला, नृत्यकला, चित्रकला एवं स्थापत्यकला में भी भारी अंतर था।
सामाजिक रीति-रिवाजों एवं सांस्कृतिक परम्पराओं के अंतर को लेकर हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे को हीन समझते थे और एक-दूसरे से घृणा करते थे। सम्पूर्ण मध्य-काल में यह समस्या बनी रही कि अपने-अपने सुदृढ़ आधारों वाली इन दो सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में सामंजस्य कैसे विकसित हो! सम्पूर्ण दिल्ली सल्तनत काल में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच की खाई गहरी तथा चौड़ी होती चली गई।
मध्य-कालीन सन्तों ने हिन्दुओं एवं मुसलमानों की बुराइयों को लेकर उनकी आलोचना की तथा लड़ने की बजाए प्रेम की साधना करने का मार्ग सुझाया। मुगल काल में अकबर ने भी हिन्दू और मुसलमानों के धर्म एवं संस्कृति में निकटता लाने के प्रयास किए। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी हिन्दू और मुस्लिम कला-परम्पराओं के समन्वय के प्रयास हुए किंतु इन दो संस्कृतियों में इतने अधिक अंतर थे कि इन्हें निकट लाना संभव नहीं हो सका।
हिन्दुओं के संस्कारों में तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना, मूर्ति-पूजा, गौ-पूजा, विष्णु-पूजा, गंगा-स्नान, रामायण एवं गीता का पाठ आदि इतने गहरे पैठ चुके थे कि वे इन बातों को छोड़ नहीं सकते थे जबकि मुसलमानों ने गौ-मांस खाना, हिन्दुओं को बलपूर्वमक मुसलमान बनाना, मंदिरों को तोड़ना आदि बातें इतनी मजबूती से पकड़ रखी थीं कि वे इन्हें छोड़कर हिन्दुओं को गले लगाने को तैयार नहीं थे।
मध्यकालीन हिन्दू रीति-रिवाज
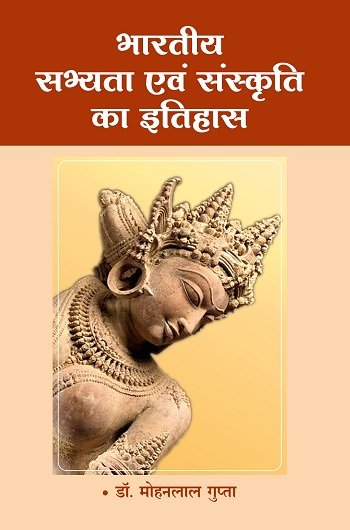
मध्यकालीन हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हिन्दू-धर्म में सोलह संस्कारों में से केवल जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, उपनयन और विवाह संस्कार आदि पांच-छः संस्कार ही प्रचलन में रह गए थे। अबुल फजल ने लिखा है कि जातकर्म संस्कार में बच्चे का जन्म होने पर घी और शहद मिलाकर सोने के छल्ले से शिशु के मुँह में डाला जाता था। बंगाल में महिलाएँ नवजात शिशु की दीर्घायु की कामना करती हुई उस पर हरी घास तथा चावल न्यौछावर करती थीं। तुलसीदास और सूरदास ने अपनी रचनाओं में शिशु जन्म के बाद होने वाले ‘नंदी मुख श्राद्ध’ का उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर ब्राह्मणों को स्वर्ण, गाय, कपड़े, भोजन आदि पदार्थ दान स्वरूप दिए जाते थे। परिवार में होने वाले मांगलिक कार्यों एवं त्यौहारों पर घर के दरवाजों पर आम या अशोक के पत्तों की बंदनवार बनाकर लटकाई जाती थे। शिशु जन्म के बाद जन्मकुंडली बनाकर उसके भविष्य के बारे में घोषणा की जाती थी। शिशु-जन्म के चालीस दिन बाद नामकरण संस्कार होता था। बंगाल में दूध, दही और हल्दी मिलाकर शिशु के ललाट पर तिलक लगया जाता था। बच्चे की रुचि जानने के लिए बच्चे के सामने धान, भात, मिट्टी, सोना, चाँदी आदि कई वस्तुएँ रख दी जाती थीं और यह देखा जाता था कि वह किसे हाथ लगाता है!
शिशु के छः माह का हो जाने पर अन्न-प्राशन्न संस्कार किया जाता था। सूरदास के पदों में आए प्रसंग के अनुसार बालक को खीर, मधु और घी चखाया जाता था जिसे उसका पिता धार्मिक अनुष्ठान के उपरान्त खिलाता था। शिशु के तीन वर्ष का होने पर मुंडन संस्कार (चूड़ाकर्म) किया जाता था तथा सिर पर एक चोटी छोड़़कर शेष बाल काट दिए जाते थे।
तभी बच्चे का कर्णच्छेदन संस्कार भी किया जाता था अर्थात् उसके दोनों कान छेदे जाते थे। आठ वर्ष की आयु में बच्चे का जनेऊ संस्कार किया जाता था जिसे उपनयन संस्कार भी कहते थे। जनेऊ में तीन सूत होते थे जिसमें प्रत्येक सूत तीन धागों को बुनकर बनाया जाता था। जनेऊ बालक के बाएं कन्धे पर लटकाया जाता था तथा जिसके छोर दाएं हाथ में लपेट दिए जाते थे।
जनेऊ के तीन सूत- ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं तथा उसका सफेद रंग पवित्रता का सूचक है। जनेऊ धारण करने के बाद बालक अपना अध्ययन प्रारम्भ करता था। विद्याध्ययन आरम्भ करने से पहले बालक को गुरु द्वारा गायत्री मंत्र सुनाया जाता था। इस अवसर पर ब्राह्मणों को दक्षिणा एवं निर्धनों को दान दिया जाता था। बालक के विद्याध्ययन की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार किया जाता था।
हिन्दुओं में विवाह की पम्पराएं एवं नियम
मध्यकालीन हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हिन्दुओं में विवाह समारोह आज की ही तरह बड़ी धूम-धाम से होते थे। हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों में बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित थी। असम में केवल ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों में बाल-विवाह का प्रचलन था। शेष जातियों में वयस्क होने पर ही विवाह होते थे। असम के अतिरिक्त शेष भारत में हिन्दुओं में बेटी का विवाह छः से आठ वर्ष की आयु तक कर दिया जाता था।
मध्यकालीन हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार अधिक उम्र की लड़कियों का पिता के घर में रहना वर्जित माना जाता था। बाल-विवाह की स्थिति में सहवास युवा होने पर ही होता था। अकबर ने विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की। विवाह के लिए दुल्हा और दुल्हन के साथ-साथ माता-पिता की सहमति भी अनिवार्य थी। अकबर के पश्चात् किसी बादशाह ने इस आदेश का समुचित पालन नहीं करवाया।
हिन्दुओं में रक्त सम्बन्धियों एवं सगोत्रियों के साथ और अन्तर्जातीय विवाहों का निषेध था। अकबर निकट रिश्तेदारों में विवाह का समर्थक नहीं था। उसने किसी नवयुवक द्वारा धन के लोभ में अधेड़ आयु की महिला से विवाह करने की प्रथा को भी गलत माना। अकबर ने आदेश दिया कि यदि स्त्री अपने पति से 12 वर्ष से अधिक बड़ी है तो ऐसा विवाह गैर-कानूनी और रद्द माना जाएगा।
मध्यकालीन हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार समाज में दहेज प्रथा प्रचलित थी। अमीर लोग अपनी पुत्री के विवाह में बहुत सा धन दहेज के रूप में दिया करते थे। निर्धन लोग भी इस प्रथा से बचे हुए नहीं थे। महाराष्ट्र के महान् सन्त तुकाराम को भी अपनी बेटी के विवाह के लिए गाँव के लोगों से धन मांगना पड़ा था। अकबर दहेज प्रथा का विरोधी था किन्तु उसने इस बुराई को समाप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया।
पिता द्वारा पुत्री को दहेज दिए जाने के साथ-साथ, मामा द्वारा भांजी के विवाह में मायरा (भात) भरने की प्रथा प्रचलित थी। नरसी मेहता को अपनी दोहिती के विवाह में मायरा भरने के लिए ईश्वर से करुण पुकार लगानी पड़ी थी।
मध्य-काल में प्रारम्भ में कुछ निम्न जातियों को छोड़कर शेष हिन्दू समाज में विधवा-विवाह पर प्रतिबंध था। किसी भी मध्य-कालीन शासक ने इसे पुनः प्रचलित करने का प्रयास नहीं किया। फलस्वरूप मध्य-काल में बाल-विधवाओं की समस्या विकट थी, जिन्हें घर की चार-दीवारी में रहते हुए नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। अकबर ने विधवा-विवाह को कानूनी घोषित किया। उसका मानना था कि जो नवयुवती अपने पति के साथ सुखभोग नहीं कर सकी है, उसे सती नहीं किया जाना चाहिए, उसका विवाह किसी विधुर से कर दिया जाना चाहिए।
हिन्दुओं में विवाह समरोह
मध्यकालीन हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हिन्दुओं में वर-वधू का चुनाव माता-पिता या घर के बड़े सदस्यों द्वारा किया जाता था। विवाह सम्बन्ध के मामले में लड़के की बात सुनी जाती थी किन्तु लड़कियों को अपने विवाह के बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था। धनी घरों की लड़कियां इसका अपवाद थीं। कुछ पुरोहित या पुरोहितिनियां या चतुर महिलाएं विवाह-योग्य लड़के-लड़कियों की जानकारी रखती थीं तथा विवाह के लिए परामर्श और सहयोग करती थीं।
जब दोनों पक्ष विवाह सम्बन्ध के लिए सहमत हो जाते थे तब ज्योतिषियों द्वारा बताए गए शुभ-मुहूर्त के दिन सगाई का दस्तूर किया जाता था। इसमें वर के माथे पर तिलक लगाकर कुछ भेंट दी जाती थीं। यद्यपि हिन्दुओं में विवाह के धार्मिक कृत्य में जाति और प्रान्त के अनुसार काफी अन्तर था तथापि धार्मिक संस्कार एक जैसे थे। समकालीन साहित्यिक ग्रन्थों में इन विवाहों के धार्मिक कृत्यों का विवरण मिलता है।
दूल्हा सुन्दर वस्त्र धारण करके अश्व पर सवार होता था, जिसके पीछे उसकी सहायता के लिए एक वयस्क पुरुष बैठता था। दूल्हे के साथ सजी हुई बारात दुल्हन के घर जाती थी। बारात के आगे रंग-बिरंगे कपड़ों में सजे बाजे वाले चलते थे, जिनके हाथों में अस्त्र-शस्त्र भी होते थे। बारात में मित्र और सम्बन्धी सम्मिलित होते थे। बारात के वधू-पक्ष के घर पहुँचने पर स्वागत किया जाता था और व्यंजन परोसे जाते थे जिसे ज्यौनार कहा जाता था।
वर और वधू एक-दूसरे को माला पहनाते थे। पुरोहितों द्वारा वैदिक मन्त्र उच्चारित किए जाते थे और अग्निकुण्ड में आहुतियां देकर देवताओं का आह्वान किया जाता था। वर-वधू उस अग्निकुण्ड के चारों ओर सात फेरे लेते थे। वधू के पिता द्वारा कन्यादान किया जाता था। वधू को लाल चूड़ियां पहनाई जाती थीं और उसकी मांग में सिंदूर भरा जाता था। वधू का पिता वर तथा उसके सम्बन्धियों को नकद, स्वर्ण तथा वस्त्र के रूप में उपहार देता था।
इसके बाद वर अपनी वधू को लेकर अपने पिता के घर आता था। अकबर ने आदेश जारी किए कि अमीर-उमराव शादी में मुबारकबाद के रूप में केवल दो नारियल भेंट करें। एक तो उस अधिकारी की ओर से तथा दूसरा बादशाह सलामत की ओर से माना जाएगा।
हिन्दुओं में विवाह विच्छेद
मध्यकालीन हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हिन्दू किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता था कई बार विभिन्न कारणों से पति-पत्नी अलग रहते थे किंतु उनमें विवाह विच्छेद की कोई कानूनी, सामाजिक या धार्मिक रीति नहीं थी।
हिन्दुओं के मृतक संस्कार
मध्यकालीन हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हिन्दुओं में अंतिम संस्कार का बड़ा महत्त्व था, क्योंकि वे इहलोक से परलोक को अधिक मान्यता देते थे। इनके मुख्य अनुष्ठान दाह-संस्कार, उदकर्म, असौच, अस्थि-संचयन, शान्ति-कर्म और सपिंडी कर्म थे। अबुल फजल ने कुछ ऐसे वर्गों का उल्लेख किया है जिनके लिए दाह-संस्कार वर्जित था। धर्मशास्त्र के अनुसार छोटे बच्चों और तपस्वियों के लिए भू-समाधि एवं जल-समाधि का प्रावधान था।
जब व्यक्ति मरणासन्न हो जाता था तब उसे चारपाई से उठाकर जमीन पर लिटा देते थे। उसका सिर उत्तर की तरफ रहता था तथा उस पर हरी दूब बिखेर कर गाय का गोबर लगाते थे। उसके मस्तक पर पवित्र गंगाजल डालकर मुँह में तथा वक्षस्थल पर तुलसीदल रखते थे। मरणासन्न व्यक्ति को भवसागर पार कराने के उद्देश्य से गोदान किया जाता था।
अन्न, वस्त्र एवं, भोजन एवं सिक्के दान किए जाते थे। अबुल फजल ने बंगाल की एक प्रथा का उल्लेख किया है, इसमें मृत्युशैय्या पर पड़े व्यक्ति को उठाकर निकट की नदी में ले जाया जाता था और मृत्यु के समय उसके शरीर को कमर तक जलधार में डुबाये रखते थे। सिक्ख-पंथ के संस्थापक गुरुनानक ने उल्लेख किया है कि किसी सम्बन्धी की मृत्यु की सूचना देने वाले पत्र के ऊपरी कौने को फाड़ दिया जाता था।
यह प्रथा आज भी प्रचलित है। मृत्यु के पश्चात् तीन दिन तक परिवार के सदस्य भूमि पर सोते थे, दिन में मांगकर या खरीद कर लाए गए भोजन ग्रहण करते थे। घर में भोजन नहीं बनाया जाता था। मृतक के परिवार वाले दस दिन से लेकर एक माह का शोक रखते थे। इस दौरान वे हजामत बनाने, वेद-पाठ करने, देव-प्रतिमाओं की पूजा करने आदि का निषेध रखते थे। गहरे रंग के कपड़े नहीं पहने जाते थे।
मध्यकालीन हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार औरतें सिर पर सफेद दुपट्टा रखती थीं। चार से दस दिन में ‘अस्थि-संचयन’ किया जाता था जिसमें चिता से राख एवं अस्थियों को एकत्रित करके दूध तथा गंगाजल से धोया जाता था और पवित्र नदियों में विसर्जित कर दिया जाता था। मृत्यु के तेरहवें दिन रिश्तेदारों द्वारा मृतक के उत्तराधिकारी को पगड़ी बांधते थे। अबुल फजल के अनुसार मृत्यु के एक साल बाद मृतक का श्राद्ध किया जाता था जिसमें ब्राह्मणों को दान दिया जाता था।
मुख्य लेख : मध्यकालीन भारतीय समाज
मध्यकालीन हिन्दू रीति रिवाज




