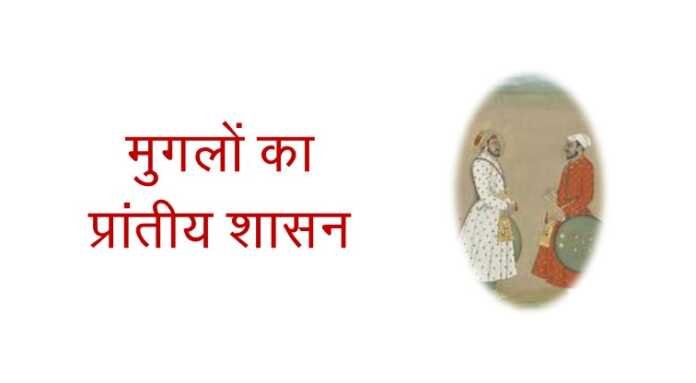मुगलों का प्रांतीय शासन पूर्ववर्ती तुर्कों द्वारा स्थापित प्रांतीय शासन की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ था। विद्रोह करने वाले प्रांतपतियों का सख्ती से दमन किया जाता था।
बाबर एवं हुमायूँ ने प्रान्तीय व्यवस्था स्थापित करने में कोई विशेष योगदान नहीं दिया। इसलिये सल्तनत कालीन व्यवस्था ही चलती रही। अकबर के शासनकाल मंे मुगल सल्तनत को सूबों (प्रान्तों) में बांटा गया। आइने अकबरी ने इनकी संख्या 12 बताई है। 1599 ई. तक बरार, खानदेश और अहमदनगर की विजय से तीन सूबे और बढ़ गये।
इस प्रकार, अकबर के शासन के अन्त में मुगलों का प्रांतीय शासन 15 सूबों में विभाजित था। जहाँगीर के समय में यही संख्या बनी रही परन्तु शाहजहाँ द्वारा थट्टा, उड़ीसा और काश्मीर को स्वतंत्र सूबे बना देने से सूबों की संख्या बढ़कर 18 हो गई। औरंगजेब द्वारा बीजापुर और गोलकुण्डा की विजय से दो सूबे और बढ़ गये।
सूबों का क्षेत्रफल स्थायी नहीं होता था। केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहते थे। प्रान्तों की आय में भी कोई समानता नहीं थी। साधारणतः समस्त सूबे बराबर थे किन्तु सुरक्षा और सामरिक महत्त्व की दृष्टि से कुछ सूबों पर अन्यों की तुलना में अधिक ध्यान दिया जाता था।
मुगलों का प्रांतीय शासन
सूबेदार
मुगलों का प्रांतीय शासन उनकी केन्द्रीय शासन व्यवस्था से मिलता-जुलता था। जदुनाथ सरकार उसे केन्द्रीय व्यवस्था का लघु रूप ही मानते हैं। प्रान्त का सर्वोच्च अधिकारी सिपहसालार तथा सूबा-ए-साहिब कहलाता था। यह पदाधिकारी सूबे में बादशाह का ही प्रतिरूप था। उसकी नियुक्ति बादशाह द्वारा की जाती थी।
सामान्यतः यह पद राजवंश के सदस्यों तथा उच्च मनसबदारों को दिया जाता था। सूबेदार की नियुक्ति और पदोन्नति के सम्बन्ध में निश्चित नियम नहीं थे। सूबेदार की नियुक्ति एक सूबे में कितने समय तक रहेगी, इसके भी स्पष्ट नियम नहीं थे। सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के बाद उनका स्थानान्तरण किया जाता था।
मुगल बादशाह की भाँति सूबेदार का अपना दरबार होता था। वह एक विशाल सेना रखता था। सूबेदार के मुख्य कामों में प्रान्त में शान्ति एवं व्यवस्था को कायम रखना, शाही आदेशों का पालन करवाना, प्रान्त से राजस्व वसूली के कार्य में सहयोग देना, विद्रोहों का दमन करना, न्याय प्रदान करना और जन-सुविधा का ध्यान रखना शामिल था।
सूबेदार के लिये ऐसे कार्य करने की मनाही थी जो बादशाह के विशेषाधिकार में थे, जैसे- चमड़ी उधड़वाना, हाथी के पैरों से कुचलवाना, झरोखा-दर्शन देना आदि। मृत्युदण्ड के मामलों में उसे शाही निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता था। बादशाह की पूर्व स्वीकृति के बिना वह पड़ौसी राज्यों से युद्ध अथवा सन्धि नहीं कर सकता था। वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों- दीवान और सद्र को नियुक्त अथवा पदच्युत भी नहीं कर सकता था।
दीवान-ए-सूबा
प्रान्तीय शासन व्यवस्था का दूसरा महत्त्वपूर्ण अधिकारी दीवान-ए-सूबा था। प्रान्त में सूबेदार के पश्चात् दीवान का ही पद था। यह प्रान्त में केन्द्रीय राजस्व विभाग का प्रतिनिधि था और किसी भी तरह से सूबेदार के अधीन नहीं था। वह सूबेदार का प्रतिद्वन्द्वी था। दोनों ही एक-दूसरे पर निगरानी रखते थे। प्रान्तीय दीवान का चुनाव केन्द्रीय दीवान करता था और बादशाह उसकी नियुक्ति करता था।
दीवान का मुख्य काम प्रान्त से राजस्व वसूल करना तथा राजस्व वसूली के लिए प्रान्तीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करना था। राजस्व सम्बन्धी विवादों को निपटाना तथा कृषि की उन्नति की तरफ ध्यान देना भी उसी का काम था। उसे अपने कामों के लिए सूबेदार की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। क्योंकि दीवान के अधिकार में अलग से सैनिक नहीं होते थे। वह अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय दीवान के पास भेजता था।
सद्र-ए-सूबा
दीवान के पश्चात न्याय और धार्मिक विभाग के अध्यक्ष का पद प्रमुख था। सद्र की नियुक्ति केन्द्र के सद्र-उस-सुदूर की सिफारिश पर बादशाह द्वारा की जाती थी। वह अपने क्षेत्र में इस्लाम के हितों के प्रति उत्तरदायी था।
काजी-ए-सूबा
काजी-ए-सूबा प्रान्तों में प्रमुख न्यायाधीश था जिसकी नियुक्ति बादशाह काजी-उल-कुजात की सिफारिश पर करता था। वह दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करता था।
बख्शी-ए-सूबा
बख्शी-ए-सूबा अथवा बख्शी, प्रान्त का प्रमुख अधिकारी था। इसकी नियुक्ति मीर बख्शी की सिफारिश पर बादशाह द्वारा की जाती थी। वह सूबे के सैनिकों की देखभाल करता था। वह प्रान्त में मनसबदारों की सूची भी रखता था। प्रान्तीय बख्शी वाकियानवीस का भी कार्य करता था। उसे माह में दो बार प्रान्त की गतिविधियों की सूचना बादशाह को भेजनी पड़ती थी।
जिला शासन व्यवस्था
मुगल काल में भी प्रान्त जिलों में विभाजित थे, जो सरकार कहलाते थे। सरकार महाल या परगने में विभाजित थी। परगने का निर्माण कई गाँवों के मिलने से होता था। शाहजहाँ के समय में कुछ परगनों को मिलाकर एक अन्य इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहा जाता था। कितने परगनों को मिलाकर एक सरकार बनती थी और एक प्रान्त में कितनी सरकार होती थी, यह निश्चित नहीं था।
फौजदार
जिले के सर्वोच्च अधिकारी को फौजदार कहते थे। उसका पद और कार्य आजकल के जिला कलक्टर के समान था। वह प्रान्तीय सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। जिले में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उसके अधीन एक सैनिक टुकड़ी रहती थी।
जदुनाथ सरकार का मानना है कि फौजदार केवल प्रान्तीय सेना का एक सेनापति होता था और उसका कार्य छोटे-छोटे विद्रोहों का दमन करना, डाकुओं का उन्मूलन करना तथा राजस्व अधिकारियों को सहयोग प्रदान करना था। उसकी नियुक्ति प्रान्तीय सूबेदार की सिफारिश पर बादशाह द्वारा की जाती थी।
अमल गुजार
जिले की शासन व्यवस्था का दूसरा प्रमुख अधिकारी अमल गुजार होता था। यह मालगुजारी एकत्र करने से सम्बन्धित मुख्य अधिकारी था। इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती थी किन्तु वह प्रान्तीय दीवान के प्रति उत्तरदायी होता था। अमलदार को बेईमान और उपद्रवी किसानों के साथ कठोर व्यवहार करने के आदेश थे। सरकारी खजाने की देखभाल भी उस के अधीन थी।
बितिक्ची
अमल गुजार के अधीन बितिक्ची होता था जो भूमि और लगान सम्बन्धी कागज तैयार करता था। वह किसानोें को लगान वसूली की रसीद देता था। परगने की शासन व्यवस्था शिकदार, आमिल, पोतदार, कानूनगो और कारकून चलाते थे।
शिकदार
शिकदार परगने का मुख्य सैनिक अधिकारी होता था जो अपने क्षेत्र में शान्ति एवं व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। वह राजस्व वसूली के कार्य में भी सहयोग देता था।
आमिल
आमिल परगने का वित्त अधिकारी था। उसका मुख्य काम किसानों से लगान वसूल करना था।
पोतदार
पोतदार परगने का खजांची था। कानूनगो परगने के पटवारियों का अधिकारी था। उसका मुख्य काम लगान, भूमि और कृषि सम्बन्धी दस्तावेजों की देखभाल करना तथा उन्हें तैयार करना था।
कोतवाल
बड़े नगर की व्यवस्था के लिए एक कोतवाल होता था। उसके पास 100 पैदल सैनिक एवं 50 घुड़सवार सैनिक होते थे। कोतवाल मुख्य रूप से नगर पुलिस का अध्यक्ष होता था किन्तु साथ ही वह नगरपालिका का प्रशासन और फौजदारी के मुकदमों के लिए स्थानीय न्यायाधीश का काम भी करता था। वह नगर में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना, मूल्यों, मापतौल के बाटों का निरीक्षण करना, अपराधों को रोकना, लावारिसों की सम्पत्ति की व्यवस्था करना, बूचड़खानों, कब्रगाहों और शमशानों पर निगरानी रखना आदि कार्य भी करता था।
ग्राम शासन
मुगलों के काल में गाँवों की शासन व्यवस्था पहले की भाँति परम्परागत ग्राम पंयाचतों के द्वारा की जाती रही। गाँवों के प्रमुख अधिकारियों में मुकद्दम, पटवारी, चौकीदार आदि मुख्य थे। डॉ. परमात्माशरण के अनुसार मुस्लिम शासकों ने अपनी दूरदृष्टि और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ग्राम बिरादरी के स्थानीय शासन के मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा।
मुख्य आलेख- मुगल शासन व्यवस्था एवं संस्थाएँ
मुगलों का प्रांतीय शासन