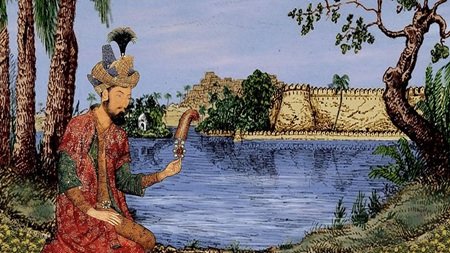हुमायूँ का पूरा नाम नासिरुद्दीन मुहम्मद हुमायूँ था। बाबर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने के बाद केवल तीन साल बाद अचानक ही मर गया था, इसलिए हुमायूँ को चारों ओर से समस्याओं ने घेर लिया।
हुमायूँ का प्रारम्भिक जीवन
बाबर के चार पुत्र और तीन पुत्रियाँ थीं जिनमें हुमायूँ सबसे बड़ा था। हुमायूँ का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। उसकी माँ माहम सुल्ताना हिरात के शिया मुसलमान हुसैन बैकरा के खानदान से थी, उसे माहिज बेगम भी कहते थे। हुमायूँ को तुर्की, अरबी, फारसी भाषओं के साथ-साथ युद्ध करने की शिक्षा भी दी गई थी।
हुमायूँ अपने पिता के जीवन काल में ही अनेक युद्धों में भाग लेने तथा प्रशासकीय कार्य करने अनुभव प्राप्त कर चुका था। उसने पानीपत तथा खनवा के युद्धों में भाग लेकर अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया था। बाबर ने उसे बंगाल तथा बिहार के अफगान अमीरों के विद्रोह का दमन करने की जिम्मेदारी दी थी।
हुमायूँ ने इस कार्य में पूरी सफलता प्राप्त की। हुमायूँ की सफलताओं से प्रसन्न होकर बाबर ने उसे दो बार बदख्शाँ का शासन प्रबन्ध सौंपा। बदख्शाँ पर उजबेग लोग बार-बार आक्रमण करते थे परन्तु हुमायूूॅँ ने उजबेगों को दबाकर वहाँ पर शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित की। बाबर ने हुमायूँ को हिसार-फिरोजा तथा सम्भल का शासन सौंपा।
हुमायूँ को आगरा के तख्त की प्राप्ति
बाबर की मृत्यु के चार दिन बाद 30 दिसम्बर 1530 को हुमायूँ आगरा के तख्त पर बैठा। इस विलम्ब का कारण यह था कि बाबर के प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली मुहम्मद खलीफा ने हुमायूँ के बहनोई मेंहदी ख्वाजा को तख्त पर बैठाने का प्रयत्न किया किंतु बाद में प्रधानमंत्री को यह अनुभव हो गया कि यदि उसने ऐसा किया तो उसका अपना जीवन खतरे में पड़ जायेगा इसलिये उसने हुमायूँ का समर्थन कर दिया।
उस समय हुमायूँ 23 वर्ष का था। उसके बादशाह बनने पर राज्य में खुशियाँ मनायी गईं और दान-दक्षिणा दी गई। राज्य के अफसरों तथा अमीरों ने उसका स्वागत किया और उसकी बादशाहत को सहर्ष स्वीकार किया। इस प्रकार हुमायूँ को तख्त प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई।
हुमायूँ की प्रारम्भिक कठिनाइयाँ
यद्यपि हुमायूँ को तख्त प्राप्त करने में विशेष कठिनाई नहीं हुई परन्तु उसका मार्ग बिल्कुल निष्कंटक नहीं था। उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ थीं जिनका निराकरण करना आवयक था-
(1.) साम्राज्य की विशालता
बाबर ने थोड़े ही दिनों में अपने सैन्यबल से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य पश्चिम में आमू नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक फैला था। दक्षिण में मालवा तथा राजपूताना के राज्य उसके साम्राज्य की सीमा पर स्थित थे। इस साम्राज्य को कुछ समय के लिये तो संभाला जा सकता था परन्तु दीर्घकालीन शासन के लिये नवीन शासन व्यवस्थायें करनी आवश्यक थीं। बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य की कोई शासकीय आधारशिला नहीं रखी गई थी।
(2.) साम्राज्य की दुर्बलता
हुमायूँ को अपने पिता से एक अव्यवस्थित राज्य मिला था। बाबर ने अपना राज्य अमीरों तथा सरदारों में बाँट दिया था जो अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी थे। ये सरदार प्रति वर्ष एक निश्चित राशि सरकारी खजाने में भेजते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर बादशाह को सैनिक सहायता उपलब्ध करवाते थे। यह सामन्तीय प्रथा हुमायूँ के लिए खतरे से खाली नहीं थी। अमीर तथा सरदार कभी भी धोखा दे सकते थे और बादशाह तथा सल्तनत के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते थे।
(3.) शासन की व्यवस्था
अभी भारत को जीतने के लिये आवश्यक युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए थे कि बाबर की मृत्यु हो गई थी इसलिये हुमायूँ जिस समय तख्त पर बैठा, वह समय युद्ध कालीन परिस्थितियों का था। अभी मुगल तथा अफगान एक दूसरे को उन्मूलित करने में संलग्न थे और उनकी सेनाओं का संचालन निरन्तर होता रहता था। ऐसी स्थिति में हुमायूँ के राज्य में बड़ी राजनीतिक तथा आर्थिक गड़बड़ी फैली हुई थी तथा शासन अस्त-व्यस्त था।
(4.) सेना का असन्तोषजनक संगठन
मुगल सेना का संगठन भी संतोषजनक नहीं था। उसमें मंगोल, उजबेग, तुर्क, चगताई, फारसी, अफगानी तथा भारतीय मुसलमान भर्ती थे। प्रत्येक सेना प्रायः अपने कबीले के नेता की अध्यक्षता में युद्ध करती थी। विभिन्न कबीलों से सम्बन्ध रखने वाली इन सेनाओं में ईर्ष्या-द्वेष व्याप्त था। इस प्रकार मुगल सेना में एकता की भावना नहीं थी। इसलिये युद्ध के समय इस सेना पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता था। कई बार सैनिक टुकड़ियां परस्पर संघर्ष करने लगती थीं। यह स्थिति राज्य के लिये अत्यंत घातक थी।
(5.) हुमायूँ के भाइयों के कुचक्र
हुमायूँ को अपने भाइयों की ओर से भी बड़ा खतरा था। हुमायूँॅ के तीन भाई थे- कामरान, अस्करी तथा हिन्दाल। इनमें से कामरान अत्यंत महत्त्वाकांक्षी था। उसमें सामरिक तथा प्रशासकीय प्रतिभा भी थी। इसलिये संभव था कि वह हुमायूँ का प्रतिद्वन्द्वी बनकर स्वयं हिन्दुस्तान का बादशाह बनने का प्रयास करे। अन्य भाई भी हुमायूँ के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न करते थे। इसलिये हुमायूँ को मंगोल शहजादों के कुचक्रों का भी सामना करना था।
(6.) अमीरों के षड्यन्त्र
अनेक मंगोल एवं चगताई अमीर शासन में अपना-अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये अलग-अलग शहजादों के समर्थक बन गये। वे इन शहजादों को हुमायूँ के विरुद्ध भड़काकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करने लगे। इससे दूर-दूर तक विस्तृत शासन को संभालना और भी कठिन हो गया।
(7.) मिर्जाओं के षड्यन्त्र
मिर्जा उन कुलीन लोगों को कहते थे जो राजवंश से सम्बन्धित होने के कारण स्वयं को तख्त का अधिकारी समझते थे। हुमायूँ को इन मिर्जाओं से उतना ही बड़ा खतरा था जितना अपने भाइयों की ओर से। राज्य में कुछ बड़े ही प्रभावशाली तथा शक्तिशाली मिर्जा विद्यमान थे जो तैमूर के वंशज थे और बाबर के तख्त के उसी प्रकार दावेदार थे जिस प्रकार बाबर के पुत्र।
इनमें सबसे अधिक प्रभावशाली मुहम्मद जमाँ मिर्जा था जिसका विवाह बाबर की पुत्री मासूमा बेगम से हुआ था। पहले वह बिहार का शासक बनाया गया परन्तु बाद में उसे जौनपुर का शासक बनाया गया जो मुगल साम्राज्य की सीमा पर स्थित था। अपने प्रभाव तथा अपनी स्थिति के कारण वह कभी भी हुमायूँ के लिए संकट उत्पन्न कर सकता था।
दूसरा प्रभावशाली मिर्जा मुहम्मद सुल्तान मिर्जा था जो सुल्तान हुसैन की लड़की का पुत्र था। हुमायूँ को इन मिर्जाओं से सतर्क रहना था क्योंकि ये लोग किसी भी संकटापन्न स्थिति में हुमायूँ के राज्य की बन्दरबांट कर सकते थे।
(8.) अफगानों की समस्या
बाबर ने पानीपत तथा घाघरा के युद्धों में अफगानों पर विजय प्राप्त कर ली थी परन्तु वह उनकी शक्ति को पूर्ण रूप से उन्मूलित नहीं कर सका था। बाबर के भय से अफगान छिन्न-भिन्न हो गये थे और उनका नैतिक बल समाप्त प्रायः था परन्तु उनमें से कई अफगान अब भी मंगोलों के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।
उन्होंने बाबर के मरते ही फिर से महमूद लोदी को अपना सुल्तान घोषित कर दिया और उसके झण्डे के नीचे संगठित होने लगे। बिबन, बयाजीद, मारूफ, फार्मूली आदि शक्तिशाली अफगान नेताओं ने अपनी सेनाओं के साथ विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया। वे अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः स्थापित करने की ताक में थे।
वे बंगाल तथा गुजरात के शासकों से मिलकर मुगलों को भारत से मार भगाने की योजनाएँ बना रहे थे। यदि हुमायूँ इन अफगानों का दमन करने का प्रयत्न करता तो उन्हें बिहार, बंगाल तथा गुजरात के शासकों से सहायता मिल सकती थी।
(9.) गुजरात के शासक बहादुरशाह की समस्या
हुमायूँ को जितना बड़ा खतरा बिहार तथा बंगाल के अफगानों से था उससे कहीं अधिक बड़ा खतरा गुजरात के शासक बहादुरशाह से था। बहादुरशाह बड़ा ही महत्त्वाकांक्षी नवयुवक था। अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उसके पास साधन भी थे। उसका राज्य बड़ा सम्पन्न था।
उस के पास हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा तोपखाना था और उसे अत्यंत योग्य अफसरों की सेवाएँ प्राप्त थीं। उसके पड़ौसी राज्य उसकी शक्ति से आतंकित रहते थे। राजपूताना, मालवा तथा दक्षिण भारत के राज्यों में बहादुरशाह का विरोध करने की क्षमता नहीं थी।
ऐसे शक्तिशाली अफगान शासक की ओर अन्य अफगान सरदारों का आकृष्ट हो जाना स्वाभाविक ही था। फतेह खाँ, कुतुब खाँ, आलम खाँ आदि कई अफगान सरदार, मुगल दरबार के कोप का भाजन बनने पर गुजरात चले गये। बहादुरशाह ने उनका स्वागत किया और उन्हें जागीरों तथा पदों से पुरस्कृत किया।
इस प्रकार बहादुरशाह हुमायूँ का बड़ा प्रतिद्वन्द्वी बन गया। उत्तर भारत में उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था और उसकी दृष्टि दिल्ली के तख्त पर थी। इसलिये हुमायूँ को उससे भी सतर्क रहना आवश्यक था।
(10.) राजपूतों की ओर से खतरा
यद्यपि बाबर ने खनवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त कर दिया था जिसका राजपूत संघ पर घातक प्रभाव पड़ा था परन्तु राणा सांगा का पुत्र रत्नसिंह फिर से अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गया था। अन्य राजपूत राज्य भी स्वयं को संगठित करने तथा अपनी शक्ति बढ़़ाने का प्रयत्न कर रहे थे।
राजपूत शासक मुगलों को घृणा की दृष्टि से देखते थे तथा वे मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिये अफगानों से गठबन्धन कर सकते थे। इसलिये हुमायूँ को उनकी ओर से भी पूरा खतरा था।
(11.) साम्राज्य विभाजन की समस्या
तुर्कों तथा मंगोलों की प्राचीन परंपरा के अनुसार बाबर की मृत्यु के उपरान्त उसका साम्राज्य उसके पुत्रों में विभक्त हो जाना चाहिए था। यदि हुमायूँ इस परम्परा की उपेक्षा करके सारा राज्य अपने अधिकार में रखने का प्रयत्न करता तो सम्भव था कि उसके भाई उनके विरुद्ध विद्रोह कर देते और अमीर लोग उनके साथ एकत्रित होकर उनका समर्थन करते।
अतः हुमायूँ ने अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने पिता का साम्राज्य अपने भाइयों में बांट दिया। उसने कामरान को पंजाब, काबुल, तथा बदख्शाँ, अस्करी को सम्भल तथा हिन्दाल को अलवर का राज्य दे दिया। साम्राज्य का शेष भाग हुमायूँ ने अपने पास रखा।
इस प्रकार हुमायूँ ने अपने पिता के साम्राज्य को अपने भाइयों में बाँट दिया परन्तु सिद्धान्तः वह अपने पिता के तख्त का उत्तराधिकारी बना रहा और उसकी प्रभुत्व शक्ति अविभक्त बनी रही। कामरान इस व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं हुआ और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए योजनाएँ बनाने लगा।
मूल आलेख – मुगल सल्तनत की अस्थिरता का युग
हुमायूँ और उसकी समस्याएँ