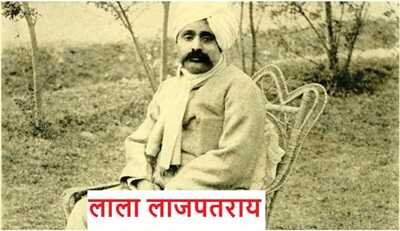उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व का मूल्यांकन करते समय हमें उनकी सफलताओं एवं विफलताओं दोनों पर विचार करना चाहिए। उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को उदारवादी नेतृत्व के दौर से आगे बढ़ाया जिसके कारण कांग्रेस को जनता का प्रबल समर्थन प्राप्त हो सका।
उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व का मूल्यांकन
उग्रवादियों की सफलताएँ
उग्रवादी आन्दोलन का प्रमुख क्षेत्र बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब था परन्तु इसका प्रभाव सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में व्याप्त था। उग्रवादी अथवा गरम दल नेताओं ने भारत के राजनीतिक जीवन में नये युग का सूत्रपात किया।
उन्होंने उदारवादियों की समझौतावादी राजनीति और ब्रिटिश न्यायप्रियता तथा ईमानदारी में विश्वास की नीति का परित्याग करके संघर्ष की नीति को अपनाया। उन्होंने भारतीय नवयुवकों में नवीन उत्साह का संचार किया तथा उनको आत्म-निर्भरता, आत्म-विश्वास और आत्म-बलिदान की शिक्षा दी।
उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को जन-आन्दोलन में बदलने का प्रयास किया। इस कारण भारत के श्रमिक, किसान, शिक्षित बेरोजगार नवयुवक, असन्तुष्ट निम्न मध्यम वर्ग, कम वेतन पाने वाले बुद्धिजीवी तथा अन्य व्यवसायों में लगे लोग इस आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए। उग्रवादियों ने ही इस बात को जोर देकर कहा कि राजनीतिक आजादी ही राष्ट्र का जीवन है।
उग्रवादियों की विफलताएँ
उग्र राष्ट्रवादी नेताओं की सफलताएं बहुत बड़ी थीं किंतु उन्हें कुछ असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। इनमें से कुछ असफलताएँ इस प्रकार से हैं-
(1.) उग्रवादियों ने भारतीय जन साधारण को आंदोलन का सही मार्ग तो दिखा दिया परन्तु वे जनता के उत्साह को संगठित आन्दोलन का रूप नहीं दे पाये।
(2.) 1907-1916 ई. की अवधि में, उदारवादियों का मनोबल गिरा हुआ था किंतु फिर भी उग्रवादी नेता न तो कांग्रेस पर कब्जा कर पाये और न ही उसके स्थान पर कोई नया लोकप्रिय दल बनाकर अपने संगठन का कौशल दिखा पाए।
(4.) उदारवादियों के विफल होते ही, ब्रिटिश सरकार ने पूरी ताकत के साथ उग्रवादियों की गतिविधियों को कुचलना आरम्भ कर दिया। 1908 ई. में समाचार पत्रों का मुंह बन्द करने के लिए समाचार पत्र विधेयक लागू किया गया, आतंकवादी अभियोगों से निपटने के लिए दंडविधि संशोधन अधिनियम (1908) लागू किया गया और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को प्रतिबंधित करने के लिए राजद्रोह सम्मेलन अधिनियम-1911 लागू किया गया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय तथा अन्य उग्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया जिससे उग्रवादियों को भारी धक्का लगा। रिहाई के बाद इनमें से बहुत से नेताओं का मनोबल टूट गया।
(4.) 1916 ई. में तिलक, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की एकता फिर से स्थापित करने में सफल रहे और एनीबीसेंट के साथ मिलकर होमरूल आन्दोलन चलाते रहे। जब 1919 ई. में मोहनदास गांधी ने असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव रखा तो तिलक और एनीबीसेंट ने कांग्रेस छोड़ दी।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उग्रवादी अथवा राष्ट्रवादी कांग्रेसी नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी किंतु उग्रवादी नेताओं के विरुद्ध उदारवादी नेताओं के अड़ियल रुख तथा उग्रवादी नेताओं का अंग्रेजी सरकार द्वारा किये गये दमन के कारण उग्रवादी नेता अधिक सफलताएँ अर्जित नहीं कर पाये।
मुख्य आलेख – उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन – गरमपंथी कांग्रेस
कांग्रेस का उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व
उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व की उत्पत्ति के कारण
उग्रराष्ट्रवादियों द्वारा बंग-भंग का विरोध
उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्व का मूल्यांकन