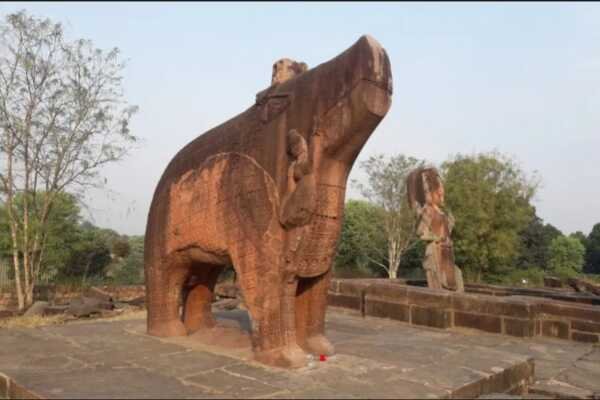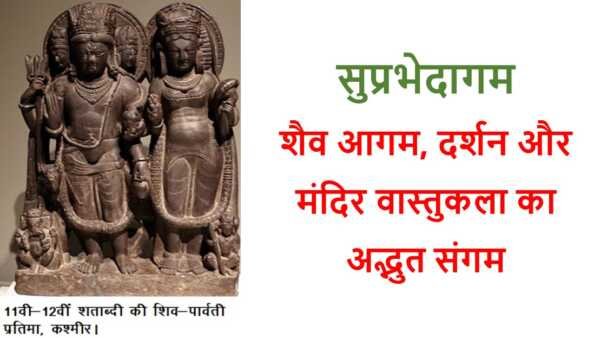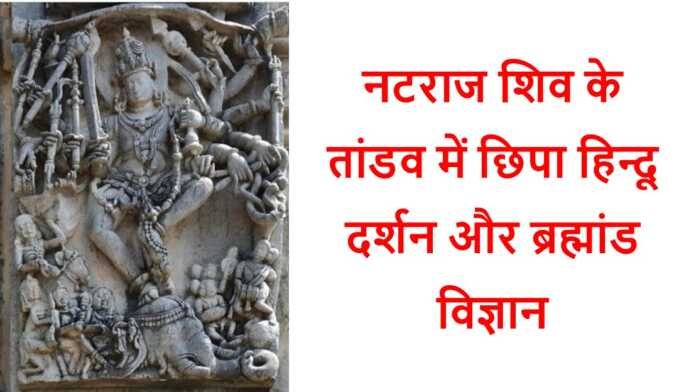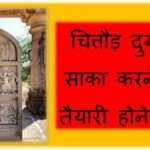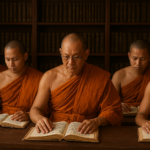मूलतः शक्ति-पूजा एवं शिल्पशास्त्र पर केन्द्रित ग्रंथ अपराजितपृच्छा विविध विषयों की जानकारी देता है। अन्य विषयों के साथ-साथ, अपराजितपृच्छा में बावड़ी वर्णन बड़े विस्तार से हुआ है।
बावड़ी – शक देश का कुंआ
बावड़ी को संस्कृत में वापी भी कहा जाता है। यह वस्तुतः सीढ़ीदार कुआं (Stepwells) होताहै। डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल का अनुमान है कि शक अपने साथ रहट और बावड़ी नामक दो विशेष प्रकार के कुएं भारत में लाए थे। बावड़ी (संस्कृत में वापी, गुजराती में बाव) के लिये प्राचीन नाम शकन्धु (शक देश का कुंआ) और रहट के लिये कर्कन्धु (कर्क देश का कुंआ) थे। कर्कदेश ईरान के दक्षिण पश्चिम में था। सातवीं शताब्दी ईस्वी के लेखक बाणभट्ट ने भी ‘हर्षचरित’ में रहट शब्द का प्रयोग किया है। राजस्थान के प्राचीन शिलालेखों में अरहट्ट भी इसी का द्योतक है।
जयपुर क्षेत्र में नगर नामक प्राचीन स्थल के वि.सं.741 (ई.684) के शिलालेख में एक वापी निर्माण का श्रेय मारवाड़ भीनमाल के कुशल शिल्पियों को दिया गया है और उन वास्तुविद्या विशारद सूत्रधारों की पर्याप्त प्रशंसा भी की गई है कि वे तो वास्तुविद्या के प्रगाढ़ पण्डित थे। सातवीं शती की यह वापी आजतक ज्ञात प्राचीनतम वापी है। मारवाड़ में वापी और रहट दोनों ही विदेशी सम्पर्क के कारण प्रचलित हुए।
बीसवीं सदी के अंत तक भी राजस्थान के कुछ भागों में मृदभाण्डों वाले रहटों का प्रयोग किया जाता था। यही स्थिति बावड़ी की भी है। बहुत सी प्राचीन बावड़ियां आज भी जल प्राप्ति हेतु काम में ली जा रही हैं। भीनमाल के चण्डीनाथ मंदिर परिसर में एक पूर्वमध्य युगीन आयताकार वापी आज भी स्थित है।
यद्यपि बावड़ी निर्माण की कला विदेशी भूमि से आई थी तथापि यह भारत में इतनी लोकप्रिय हुई कि मध्यकाल आते-आते यह हिन्दू संस्कृति की प्रतीक बन गई।
अपराजितपृच्छा में बावड़ी वर्णन
अपराजितपृच्छा में बावड़ियों का वर्णन अत्यंत वैज्ञानिक और विस्तृत है। पश्चिम भारत, विशेषकर गुजरात और राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए इन संरचनाओं का निर्माण एक आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य माना जाता था।
भुवनदेवाचार्य ने इस ग्रंथ में बावड़ियों के वर्गीकरण, उनके माप और निर्माण की सूक्ष्म विधियों का उल्लेख किया है।
अपराजितपृच्छा में बावड़ी वर्णन – चार मुख्य प्रकार
ग्रंथ में प्रवेश द्वारों की संख्या के आधार पर बावड़ियों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- नंदा (Nanda): इसमें केवल एक प्रवेश द्वार और एक कूट (Pavilion) होता है। यह सबसे सरल संरचना है।
- भद्रा (Bhadra): इसमें दो प्रवेश द्वार होते हैं। यह मध्य आकार की बावड़ी होती है जिसमें विश्राम के लिए अधिक स्थान होता है।
- जया (Jaya): इसमें तीन प्रवेश द्वार होते हैं। यह काफी विशाल और भव्य होती है।
- विजया (Vijaya): इसमें चार प्रवेश द्वार होते हैं। यह सबसे दुर्लभ और राजसी प्रकार की बावड़ी है, जो स्थापत्य कला का शिखर मानी जाती है।
अपराजितपृच्छा में बावड़ी वर्णन – प्रमुख सिद्धांत और विशेषताएं
1. कूट और सोपान (Pavilions and Steps):
ग्रंथ के अनुसार, बावड़ी केवल जमीन में खोदा गया गड्ढा नहीं है, अपितु एक बहुमंजिला भूमिगत भवन है। इसमें सीढ़ियों के बीच-बीच में कूट (मंडप) बनाए जाते हैं, जो मिट्टी के दबाव को रोकने के साथ-साथ राहगीरों के बैठने के काम आते थे।
2. मान और प्रमाण (Measurement):
ग्रंथ में बावड़ी की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का एक निश्चित अनुपात दिया गया है। यदि यह अनुपात सही न हो, तो संरचना के ढहने का भय रहता था। इसमें हस्त (हाथ की लंबाई) को मानक इकाई माना गया है।
3. जल का आध्यात्मिक महत्व:
अपराजितपृच्छा के अनुसार, जल के भीतर देवताओं का वास होता है। इसलिए, बावड़ी की दीवारों पर वराह, विष्णु, लक्ष्मी और गंगा-यमुना की मूर्तियां उकेरी जाती थीं। रानी की वाव (पाटन) इसका सबसे जीवंत उदाहरण है, जहाँ दीवारों पर लगभग 800 से अधिक मूर्तियां हैं।
4. इंजीनियरिंग और भूविज्ञान:
इसमें बताया गया है कि बावड़ी का निर्माण करते समय जल-शिरा (Aquifers) की पहचान कैसे की जाए और मिट्टी की प्रकृति के अनुसार नींव कैसे रखी जाए। यह आज के हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का प्राचीन रूप है।
सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका
इन बावड़ियों का निर्माण केवल पानी पीने के लिए नहीं, अपितु सामुदायिक केंद्रों के रूप में किया जाता था। गर्मियों के दिनों में ये भूमिगत स्थल ठंडे रहते थे, जहाँ यात्री और स्थानीय लोग समय बिताते थे। यह महिलाओं के सामाजिक मेलजोल का भी एक प्रमुख स्थान था।
👉डॉ. मोहनलाल गुप्ता द्वारा लिखित ऐतिहासिक पुस्तकें-
डॉ. मोहनलाल गुप्ता की पुस्तकें